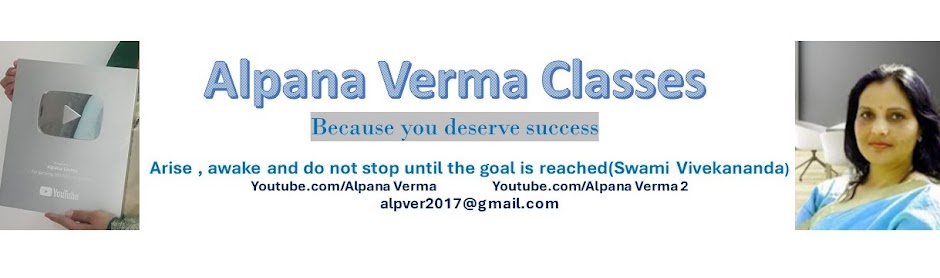Part 1
Part 2
एक दिन का मेहमान (कहानी ) /लेखक : निर्मल वर्मा
उसने अपना सूटकेस दरवाजे के आगे रख दिया। घंटी का बटन दबाया और प्रतीक्षा करने लगा। मकान चुप था। कोई हलचल नहीं – एक क्षण के लिए भ्रम हुआ कि घर में कोई नहीं है और वह खाली मकान के आगे खड़ा है। उसने रूमाल निकाल कर पसीना पोंछा, अपना एयर-बैग सूटकेस पर रख दिया। दोबारा बटन दबाया और दरवाजे से कान सटा कर सुनने लगा, बरामदे के पीछे कोई खुली खिड़की हवा में हिचकोले खा रही थी।
वह पीछे हट कर ऊपर देखने लगा। वह दुमंजिला मकान था – लेन के अन्य मकानों की तरह-काली छत, अंग्रेजी ‘वी’ की शक्ल में दोनों तरफ से ढलुआँ, और बीच में सफेद पत्थर की दीवार, जिसके माथे पर मकान का नंबर एक काली बिंदी-सा टिमक रहा था। ऊपर की खिड़कियाँ बंद थीं और परदे गिरे थे। कहाँ जा सकते हैं इस वक्त?
वह मकान के पिछवाड़े गया – वही लॉन, फेंस और झाड़ियाँ थीं, जो उसने दो साल पहले देखी थीं, बीच में विलो अपनी टहनियाँ झुकाए एक काले, बूढ़े रीछ की तरह ऊँघ रहा था। लेकिन गैराज खुला और खाली पड़ा था; वे कहीं कार ले कर गए थे, संभव है, उन्होंने सारी सुबह उसकी प्रतीक्षा की हो और अब किसी काम से बाहर चले गए हों। लेकिन दरवाजे पर उसके लिए एक चिट तो छोड़ ही सकते थे?
वह दोबारा सामने के दरवाजे पर लौट आया। अगस्त की चुनचुनाती धूप उनकी आँखों पर पड़ रही थी। सारा शरीर चू रहा था। वह बरामदे में ही अपने सूटकेस पर बैठ गया। अचानक उसे लगा, सड़क के पार मकानों की खिड़कियों से कुछ चेहरे बाहर झाँक रहे हैं, उसे देख रहे हैं। उसने सुना था, अंग्रेज लोग दूसरों की निजी चिंताओं में दखल नहीं देते, लेकिन वह मकान के बाहर बरामदे में बैठा था, जहाँ प्राइवेसी का कोई मतलब नहीं था; इसलिए वे निस्संकोच, नंगी उन्मुक्तता से उसे घूर रहे थे। लेकिन शायद उनके कौतूहल का एक दूसरा कारण था; उस छोटे, अंग्रेजी कस्बाती शहर में लगभग सब एक-दूसरे को पहचानते थे और वह न केवल अपनी शक्ल-सूरत में, बल्कि झूलते-झालते हिंदुस्तानी सूट में काफी अद्भुत प्राणी दिखाई दे रहा होगा। उसकी तुड़ी-मुड़ी वेशभूषा और गर्द और पसीने में लथपथ चेहरे से कोई यह अनुमान भी नहीं लगा सकता था कि अभी तीन दिन पहले फ्रेंकफर्ट की कान्फ्रेंस में उसने पेपर पढ़ा था।
‘मैं एक लुटा-पिटा एशियन इमीग्रेंट दिखाई दे रहा हूँगा’ …उसने सोचा और अचानक खड़ा हो गया-मानो खड़ा हो कर प्रतीक्षा करना ज्यादा आसान हो। इस बार बिना सोचे-समझे उसने दरवाजा जोर से खटखटाया और तत्काल हकबका कर पीछे हट गया – हाथ लगते ही दरवाजा खट-से खुल गया। जीने पर पैरों की आवाज सुनाई दी – और दूसरे क्षण वह चौखट पर उसके सामने खड़ी थी।
वह भागते हुए सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आई थी, और उससे चिपट गई थी। इससे पहले वह पूछता, क्या तुम भीतर थीं? और वह पूछती, तुम बाहर खड़े थे? – उसने अपने धूल-भरे लस्तम-पस्तम हाथों से उसके दुबले कंधों को पकड़ लिया और लड़की का सिर नीचे झुक आया और उसने अपना मुँह उसके बालों पर रख दिया।
पड़ोसियों ने एक-एक करके अपनी खिड़कियाँ बंद कर दीं।
लड़की ने धीरे से उसे अपने से अलग कर दिया, ‘बाहर कब से खड़े थे?’
‘पिछले दो साल से।’
‘वाह!’ लड़की हँसने लगी। उसे अपने बाप की ऐसी ही बातें बौड़म जान पड़ती थीं।
‘मैंने दो बार घंटी बजाई – तुम लोग कहाँ थे?’
‘घंटी खराब है, इसलिए मैंने दरवाजा खुला छोड़ दिया था।’
‘तुम्हें मुझे फोन पर बताना चाहिए था – मैं पिछले एक घंटे से आगे-पीछे दौड़ रहा था।’
‘मैं तुम्हें बतानेवाली थी, लेकिन बीच में लाइन कट गई… तुमने और पैसे क्यों नहीं डाले?’
‘मेरे पास सिर्फ दस पैसे थे… वह औरत काफी चुड़ैल थी।’
‘कौन औरत?’ लड़की ने उसका बैग उठाया।
‘वही, जिसने हमें बीच में काट दिया।’
आदमी अपना सूटकेस बीच ड्राइंगरूम में घसीट लाया। लड़की उत्सुकता से बैग के भीतर झाँक रही थी – सिगरेट के पैकेट, स्कॉच की लंबी बोतल, चॉकलेट के बंडल – वे सारी चीजें, जो उसने इतनी हड़बड़ी में फ्रेंकफर्ट के एयरपोर्ट पर ड्यूटी-फ्री दुकान से खरीदी थीं, अब बैग से ऊपर झाँक रही थीं।
‘तुमने अपने बाल कटवा लिए?’ आदमी ने पहली बार चैन से लड़की का चेहरा देखा।
‘हाँ… सिर्फ छुट्टियों के लिए। कैसे लगते हैं?’
‘अगर तुम मेरी बेटी नहीं होतीं तो मैं समझता, कोई लफंगा घर में घुस आया है।’
‘ओह, पापा!’ लड़की ने हँसते हुए बैग से चाकलेट निकाली, रैपर खोला, फिर उसके आगे बढ़ा दी।
‘स्विस चाकलेट,’ उसने उसे हवा में डुलाते हुए कहा।
‘मेरे लिए एक गिलास पानी ला सकती हो?’
‘ठहरो, मैं चाय बनाती हूँ।’
‘चाय बाद में…’ वह अपने कोट की अंदरूनी जेब में कुछ टटोलने लगा – नोटबुक, वालेट, पासपोर्ट – सब चीजें बाहर निकल आईं, अंत में उसे टेबलेट्स की डिब्बी मिली, जिसे वह ढूँढ़ रहा था।
लड़की पानी का गिलास ले कर आई तो उससे पूछा, ‘कैसी दवाई है?’
‘जर्मन,’ उसने कहा, ‘बहुत असर करती है।’ उसने टेबलेट पानी के साथ निगल ली, फिर सोफे पर बैठ गया। सब कुछ वैसा ही था, जैसा उसने सोचा था। वही कमरा, शीशे का दरवाजा, खुले हुए परदों के बीच वही चौकोर, हरे रूमाल-जैसा लॉन, टी.वी. के स्क्रीन पर उड़ती पक्षियों की छाया, जो बाहर उड़ते थे और भीतर होने का भ्रम देते थे…।
वह किचन की देहरी पर आया। गैस के चूल्हों के पीछे लड़की की पीठ दिखाई दे रही थी। कार्डराय की काली जींस और सफेद कमीज, जिसकी मुड़ी स्लीव्स बाँहों की कुहनियों पर झूल रही थीं। वह बहुत हल्की और छुई-मुई-सी दिखाई दे रही थी।
‘मामा कहाँ हैं?’ उसने पूछा। शायद उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि लड़की ने उसे नहीं सुना, किंतु उसे लगा, जैसे लड़की की गर्दन कुछ ऊपर उठी थी। ‘मामा क्या ऊपर हैं?’ उसने दोबारा कहा और लड़की वैसे ही निश्चल खड़ी रही और तब उसे लगा, उसने पहली बार भी उसके प्रश्न को सुन लिया था। ‘क्या वह बाहर गई हैं?’ उसने पूछा। लड़की ने बहुत धीरे, धुँधले ढंग से सिर हिलाया, जिसका मतलब कुछ भी हो सकता था।
‘तुम पापा, कुछ मेरी मदद करोगे?’
वह लपक कर किचन में चला आया, ‘बताओ, क्या काम है?’
‘तुम चाय की केतली ले कर भीतर जाओ, मैं अभी आती हूँ।’
‘बस!’ उसने निराश स्वर में कहा।
‘अच्छा, प्याले और प्लेटें भी लेते जाओ।’
वह सब चीजें ले कर भीतर कमरे में चला आया। वह दोबारा किचन में जाना चाहता था, लेकिन लड़की के डर से वह वहीं सोफा पर बैठा रहा। किचन से कुछ तलने की खुश्बू आ रही थी। लड़की उसके लिए कुछ बना रही थी – और वह उसकी कोई भी मदद नहीं कर पा रहा था। एक बार इच्छा हुई, किचन में जा कर उसे मना कर आए कि वह कुछ नहीं खाएगा – किंतु दूसरे क्षण भूख ने उसे पकड़ लिया। सुबह से उसने कुछ नहीं खाया था। यूस्टन स्टेशन के कैफेटेरिया में इतनी लंबी ‘क्यू’ लगी थी कि वह टिकट ले कर सीधा ट्रेन में घुस गया था। सोचा था, वह डायनिंग-कार में कुछ पेट में डाल लेगा, किंतु वह दुपहर से पहले नहीं खुलती थी। सच पूछा जाए, तो उसने अंतिम खाना कल शाम फ्रेंकफर्ट की एयरपोर्ट में खाया था और जब रात को लंदन पहुँचा था, तो अपने होटल की बॉर में पीता रहा था। तीसरे गिलास के बाद उसने जेब से नोटबुक निकाली, नंबर देखा और बॉर के टेलीफोन बूथ में जा कर फोन मिलाया था…
पहली बार में पता नहीं चला, उसकी पत्नी की आवाज है या बच्ची की। उसकी पत्नी ने फोन उठाया होगा, क्योंकि कुछ देर तक फोन का सन्नाटा उसके कान में झनझनाता रहा, फिर उसने सुना, वह ऊपर से बच्ची को बुला रही है। और तब उसने घड़ी देखी; उसे अचानक ध्यान आया, इस समय वह सो रही होगी, और वह फोन नीचे रखना चाहता था, किंतु उसी समय उसे बच्ची का स्वर सुनाई दिया; वह आधी नींद में थी। उसे कुछ देर तक पता ही नहीं चला कि वह इंडिया से बोल रहा है या फ्रेंकफर्ट से या लंदन से… वह उसे अपनी स्थिति समझा ही रहा था कि तीन मिनट खत्म हो गए और उसके पास इतनी ‘चेंज’ भी नहीं थी कि वह लाइन को कटने से बचा सके, तसल्ली सिर्फ इतनी थी कि वह नींद, घबराहट और नशे के बीच यह बताने में सफल हो गया कि वह कल उनके शहर पहँच रहा है… कल यानी आज।
वे अच्छे क्षण थे। बाहर इंग्लैंड की पीली और मुलायम धूप फैली थी। वह घर के भीतर था। उसके भीतर गरमाई की लहरें उठने लगी थीं। हवाई अड्डों की भाग-दौड़, होटलों की हील-हुज्जत, ट्रेन-टैक्सियों की हड़बड़ाहट – वह सबसे परे हो गया था। वह घर के भीतर था; उसका अपना घर न सही, फिर भी एक घर – कुर्सियाँ, परदे, सोफा, टी.वी.। वह अर्से से इन चीजों के बीच रहा था और हर चीज के इतिहास को जानता था। हर दो-तीन साल बाद जब वह आता था, तो सोचता था – बच्ची कितनी बड़ी हो गई होगी और पत्नी? वह कितनी बदल गई होगी! लेकिन ये चीजें उस दिन से एक जगह ठहरी थीं, जिस दिन उसने घर छोड़ा था; वे उसके साथ जाती थीं, उसके साथ लौट आती थीं…
‘पापा, तुमने चाय नहीं डाली?’ वह किचन से दो प्लेटें ले कर आई, एक में टोस्ट और मक्खन थे, दूसरे में तले हुए सॉसेज।
‘मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था।’
‘चाय डालो, नहीं तो बिल्कुल ठंडी हो जाएगी।’
वह उसके साथ सोफा पर बैठ गई। ‘टी.वी. खोल दूँ… देखोगे?’
‘अभी नहीं… सुनो, तुम्हें मेरे स्टैंप्स मिल गए थे?’
‘हाँ, पापा, थैंक्स!’ वह टोस्ट्स पर मक्खन लगा रही थी।
‘लेकिन तुमने चिट्ठी एक भी नहीं लिखी!’
‘मैंने एक लिखी थी, लेकिन जब तुम्हारा टेलीग्राम आया, तो मैंने सोचा, अब तुम आ रहे हो तो चिट्ठी भेजने की क्या जरूरत?’
‘तुम सचमुच गागा हो।’
लड़की ने उसकी ओर देखा और हँसने लगी। यह उसका चिढ़ाऊ नाम था, जो बाप ने बरसों पहले उसे दिया था, जब वह उसके साथ घर में रहता था, वह बहुत छोटी थी और उसने हिंदुस्तान का नाम भी नहीं सुना था।
बच्ची की हँसी का फायदा उठाते हुए वह उसके पास झुक आया जैसे कोई चंचल चिड़िया हो, जिसे केवल सुरक्षा के भ्रामक क्षण में ही पकड़ा जा सकता है, ‘ममी कब लौटेंगी?’
प्रश्न इतना अचानक था कि लड़की झूठ नहीं बोल सकी, ‘वह ऊपर अपने कमरे में हैं।’
‘ऊपर? लेकिन तुमने तो कहा था…’
किरच, किरच, किरच – वह चाकू से जले हुए टोस्ट को कुरेद रही थी मानो उसके साथ-साथ वह उसके प्रश्न को भी काट डालना चाहती हो। हँसी अब भी थी, लेकिन अब वह बर्फ में जमे कीड़े की तरह उसके होंठों पर चिपकी थी।
‘क्या उन्हें मालूम है कि मैं यहाँ हूँ?’
लड़की ने टोस्ट पर मक्खन लगाया, फिर जैम – फिर उसके आगे प्लेट रख दी।
‘हाँ, मालूम है।’ उसने कहा।
‘क्या वह नीचे आ कर हमारे साथ चाय नहीं पिएँगी?’
लड़की दूसरी प्लेट पर सॉसेज सजाने लगी – फिर उसे कुछ याद आया। वह रसोई में गई और अपने साथ मस्टर्ड और कैचुप की बोतलें ले आई।
‘मैं ऊपर जा कर पूछ आता हूँ।’ उसने लड़की की तरफ देखा, जैसे उससे अपनी कार्यवाही का समर्थन पाना चाहता हो। जब वह कुछ नहीं बोली, तो वह जीने की तरफ जाने लगा।
‘प्लीज, पापा!’
उसके पाँव ठिठक गए।
‘आप फिर उनसे लड़ना चाहते हैं?’ लड़की ने कुछ गुस्से में उसे देखा।
‘लड़ना!’ वह शर्म से भीगा हुआ हँसने लगा, ‘मैं यहाँ दो हजार मील उनसे लड़ने आया हूँ?’
‘फिर आप मेरे पास बैठिए।’ लड़की का स्वर भरा हुआ था। वह अपनी माँ के साथ थी, लेकिन बाप के प्रति क्रूर नहीं थी। वह उसे पुरचाती निगाहों से निहार रही थी, ‘मैं तुम्हारे पास हूँ, क्या यह काफी नहीं है?’
वह खाने लगा, टोस्ट, सॉसेज, टिन के उबले हुए मटर। उसकी भूख उड़ गई थी, लेकिन लड़की की आँखें उस पर थीं। वह उसे देख रही थी, और कुछ सोच रही थी, कभी-कभी टोस्ट का एक टुकड़ा मुँह में डाल लेती और फिर चाय पीने लगती। फिर उसकी ओर देखती और चुपचाप मुस्कराने लगती, उसे दिलासा-सी देती, सब कुछ ठीक है, तुम्हारी जिम्मेदारी मुझ पर है और जब तक मैं हूँ, डरने की कोई बात नहीं।
डर नहीं था। टेबलेट का असर रहा होगा, या यात्रा की थकान – वह कुछ देर के लिए लड़की की निगाहों से हटना चाहता था। वह अपने को हटाना चाहता था। ‘मैं अभी आता हूँ।’ उसने कहा। लड़की ने सशंकित आँखों से उसे देखा, ‘क्या बाथरूम जाएँगे?’ वह उसके साथ-साथ गुसलखाने तक चली आई और जब उसने दरवाजा बंद कर लिया, तो भी उसे लगता रहा, वह दरवाजे के पीछे खड़ी है…
उसने बेसिनी में अपना मुँह डाल दिया और नलका खोल दिया। पानी झर-झर उसके चेहरे पर बहने लगा – और वह सिसकने-सा लगा, आधे बने हुए शब्द उसकी छाती के खोखल से बाहर निकलने लगे, जैसे भीतर जमी हुई काई उलट रहा हो, उलटी, जो सीधी दिल से बाहर आती है – वह टेबलेट जो कुछ देर पहले खाई थी, अब पीले चूरे-सी बेसिनी के संगमरमर पर तैर रही थी। फिर उसने नल बंद कर दिया और रूमाल निकाल कर मुँह पोंछा। बाथरूम की खूँटी पर स्त्री के मैले कपड़े टँगे थे – प्लास्टिक की एक चौड़ी बाल्टी में अंडरवियर और ब्रेसियर साबुन में डूबे थे… खिड़की खुली थी और बाग का पिछवाड़ा धूप में चमक रहा था। कहीं किसी दूसरे बाग से घास कटने की उनींदी-सी घुर्र-घुर्र पास आ रही थी…
वह जल्दी से बाथरूम का दरवाजा बंद करके कमरे में चला आया। सारे घर में सन्नाटा था। वह किचन में आया, तो लड़की दिखाई नहीं दी। वह ड्राइंगरूम में लौटा, तो वह भी खाली पड़ा था। उसे संदेह हुआ कि वह ऊपरवाले कमरे में अपनी माँ के पास बैठी है। एक अजीब आतंक ने उसे पकड़ लिया। घर जितना शांत था, उतना ही खतरे से अटा जान पड़ा। वह कोने में गया, जहाँ उसका सूटकेस रखा था, वह जल्दी-जल्दी उसे खोलने लगा। उसने अपने कान्फ्रेंस के नोट्स और कागज अलग किए, उनके नीचे से वह सारा सामान निकालने लगा, जो वह दिल्ली से अपने साथ लाया था – एंपोरियम का राजस्थानी लहँगा (लड़की के लिए), ताँबे और पीतल के ट्रिंकेट्स, जो उसने जनपथ पर तिब्बती लामा हिप्पियों से खरीदे थे, पशमीने की कश्मीरी शॉल (बच्ची की माँ के लिए), एक लाल गुजराती जरीदार स्लीपर, जिसे बच्ची और माँ दोनों पहन सकते थे, हैंडलूम के बेडकवर, हिंदुस्तानी टिकटों का अल्बम – और एक बहुत बड़ी सचित्र किताब ‘बनारस : द एटर्नल सिटी।’ फर्श पर धीरे-धीरे एक छोटा-सा हिंदुस्तान जमा हो गया था जिसे वह हर बार यूरोप आते समय अपने साथ ढो लाता था।
सहसा उसके हाथ ठिठक गए। वह कुछ देर तक चीजों के ढेर को देखता रहा। कमरे के फर्श पर बिखरी हुई वे बिल्कुल अनाथ और दयनीय दिखाई दे रही थीं। एक पागल-सी इच्छा हुई कि वह उन्हें कमरे में जैसे का तैसा छोड़ कर भाग खड़ा हो। किसी को पता भी न चलेगा, वह कहाँ चला गया? लड़की थोड़ा-बहुत जरूर हैरान होगी, किंतु बरसों से वह उससे ऐसे ही अचानक मिलती रही थी और बिना कारण बिछुड़ती रही थी, ‘यू आर ए कमिंग मैन एंड ए गोइंग मैन’, वह उससे कहा करती थी, पहले विषाद में और बाद में कुछ-कुछ हँसी में… उसे कमरे में न बैठा देख कर लड़की को ज्यादा सदमा नहीं पहुँचेगा। वह ऊपर जाएगी और माँ से कहेगी, ‘अब तुम नीचे आ सकती हो; वह चले गए।’ फिर वे दोनों एक-साथ नीचे आएँगी, और उन्हें राहत मिलेगी कि अब उन दोनों के अलावा घर में कोई नहीं है।
‘पापा!’
वह चौंक गया, जैसे रँगे हाथों पकड़ा गया हो। खिसियानी-सी मुस्कराहट में लड़की को देखा – वह कमरे की चौखट पर खड़ी थी और खुले हुए सूटकेस को ऐसे देख रही थी, जैसे वह कोई जादू की पिटारी हो, जिसने अपने पेट से अचानक रंग-बिरंगी चीजों को उगल दिया हो, लेकिन उसकी आँखों में कोई खुशी नहीं थी; एक शर्म-सी थी, जब बच्चे अपने बड़ों को कोई ऐसी ट्रिक करते हुए देखते हैं जिसका भेद उन्हें पहले से मालूम होता है; वे अपने संकोच को छिपाने के लिए कुछ ज्यादा ही उत्सुक हो जाते हैं।
‘इतनी चीजें?’ वह आदमी के सामने कुर्सी पर बैठ गई, ‘कैसे लाने दीं? सुना है, आजकल कस्टमवाले बहुत तंग करते हैं!’
‘नहीं, इस बार उन्होंने कुछ नहीं किया,’ आदमी ने उत्साह में आ कर कहा, ‘शायद इसलिए कि मैं सीधे फ्रेंकफर्ट से आ रहा था। उन्हें सिर्फ एक चीज पर शक हुआ था।’ उसने मुस्कराते हुए लड़की की ओर देखा।
‘किस चीज पर?’ लड़की ने इस बार सच्ची उत्सुकता से पूछा।
उसने अपने बैग से दालबीजी का डिब्बा निकाला और उसे खोल कर मेज पर रख दिया। लड़की ने झिझकते हुए दो-चार दाने उठाए और उन्हें सूँघने लगी, ‘क्या है यह?’ उसने जिज्ञासा से आदमी को देखा।
‘वे भी इसी तरह सूँघ रहे थे,’ वह हँसने लगा, ‘उन्हें डर था कि कहीं इसमें चरस-गाँजा तो नहीं है।’
‘हैश?’ लड़की की आँखें फैल गईं, ‘क्या इसमें सचमुच हैश मिली है?’
‘खा कर देखो।’
लड़की ने कुछ दालमोठ मुँह में डाले और उन्हें चबाने लगी, फिर हलाट-सी हो कर सी-सी करने लगी।
‘मिर्चें होंगी – थूक दो!’ आदमी ने कुछ घबरा कर कहा।
किंतु लड़की ने उन्हें निगल लिया और छलछलाई आँखों से बाप को देखने लगी।
‘तुम भी पागल हो… सब निगल बैठीं।’ आदमी ने जल्दी से उसे पानी का गिलास दिया, जो वह उसके लिए लाई थी।
‘मुझे पसंद है।’ लड़की ने जल्दी से पानी पिया और अपनी कमीज की मुड़ी हुई बाँहों से आँखें पोंछने लगी। फिर मुस्कराते हुए आदमी की ओर देखा, ‘आई लव इट।’ वह कई बातें सिर्फ आदमी का मन रखने के लिए करती थी। उनके बीच बहुत कम मुहलत रहती थी और वह उसके निकट पहुँचने के लिए ऐसे शॉर्टकट लेती थी, जिसे दूसरे बच्चे महीनों में पार करते हैं।
‘क्या उन्होंने भी इसे चख कर देखा था?’ लड़की ने पूछा।
‘नहीं, उनमें इतनी हिम्मत कहाँ थी! उन्होंने सिर्फ मेरा सूटकेस खोला, मेरे कागजों को उल्टा-पलटा और जब उन्हें पता चला कि मैं कान्फ्रेंस से आ रहा हूँ तो उन्होंने कहा, ‘मिस्टर, यू मे गो।’ ‘
‘क्या कहा उन्होंने?’ लड़की हँस रही थी।
‘उन्होंने कहा, ‘मिस्टर यू मे गो, लाइक एन इंडियन क्रो!’ आदमी ने भेदभरी निगाहों से उसे देखा। ‘क्या है यह?’
लड़की हँसती रही – जब वह बहुत छोटी थी और आदमी के साथ पार्क में घूमने जाती थी, तो वे यह सिरफिरा खेल खेलते थे। वह पेड़ की ओर देख कर पूछता था, ओ डियर, इज देयर एनीथिंग टू सी? और लड़की चारों तरफ देख कर कहती थी, येस डियर, देयर इज ए क्रो ओवर द ट्री। आदमी विस्मय से उसकी ओर देखता। क्या है यह? और वह विजयोल्लास में कहती – पोयम!
ए पोयम! बढ़ती हुई उम्र में छूटते हुए बचपन की छाया सरक आई – पार्क की हवा, पेड़, हँसी। वह बाप की उँगली पकड़ कर सहसा एक ऐसी जगह आ गई, जिसे वह मुद्दत पहले छोड़ चुकी थी, जो कभी-कभार रात को सोते हुए सपनों में दिखाई दे जाती थी…
‘मैं तुम्हारे लिए कुछ इंडियन सिक्के लाया था… तुमने पिछली बार कहा था न!’
‘दिखाओ, कहाँ हैं?’ लड़की ने कुछ जरूरत से ज्यादा ही ललकते हुए पूछा।
आदमी ने सलमे-सितारों से जड़ी एक लाल थैली उठाई – जिसे हिप्पी लोग अपने पासपोर्ट के लिए खरीदते थे। लड़की ने उसे उसके हाथ से छीन लिया और हवा में झुलाने लगी। भीतर रखी चवन्नियाँ, अठन्नियाँ चहचहाने लगीं, फिर उसने थैली का मुँह खोला और सारे पैसों को मेज पर बिखेर दिया।
‘हिंदुस्तान में क्या सब लोगों के पास ऐसे ही सिक्के होते हैं?’
वह हँसने लगा, ‘और क्या सबके लिए अलग-अलग बनेंगे?’ उसने कहा।
‘लेकिन गरीब लोग?’ उसने आदमी को देखा, ‘मैंने एक रात टी.वी. में उन्हें देखा था…।’ वह सिक्कों को भूल गई और कुछ असमंजस में फर्श पर बिखरी चीजों को देखने लगी। तब पहली बार आदमी को लगा – वह लड़की जो उसके सामने बैठी है, कोई दूसरी है। पहचान का फ्रेम वही है जो उसने दो साल पहले देखा था लेकिन बीच की तस्वीर बदल गई है। किंतु वह बदली नहीं थी, वह सिर्फ कहीं और चली गई थी। वे माँ-बाप जो अपने बच्चों के साथ हमेशा नहीं रहते, उन गोपनीय मंजिलों के बारे में कुछ नहीं जानते जो उनके अभाव की नींव पर ऊपर ही ऊपर बनती रहती हैं, लड़की अपने बचपन की बेसमेंट में जा कर ही पिता से मिल पाती थी… लेकिन कभी-कभी उसे छोड़ कर दूसरे कमरों में चली जाती थी, जिसके बारे में आदमी को कुछ भी मालूम नहीं था।
‘पापा!’ लड़की ने उसकी ओर देखा, ‘क्या मैं इन चीजों को समेट कर रख दूँ?’
‘क्यों, इतनी जल्दी क्या है?’
‘नहीं, जल्दी नहीं… लेकिन मामा आ कर देखेंगी तो…!’ उसके स्वर में हल्की-सी घबराहट थी, जैसे वह हवा में किसी अदृश्य खतरे को सूँघ रही हो।
‘आएँगी तो क्या?’ आदमी ने कुछ विस्मय से लड़की की ओर देखा।
‘पापा, धीरे बोलो…!’ लड़की ने ऊपर कमरे की तरफ देखा, ऊपर सन्नाटा था, जैसे घर की एक देह हो, दो में बँटी हुई, जिसका एक हिस्सा सुन्न और निस्पंद पड़ा हो, दूसरे में वे दोनों बैठे थे। और तब उसे भ्रम हुआ कि लड़की कोई कठपुतली का नाटक कर रही है। ऊपर के धागे से बँधी हुई, जैसे वह खिंचता है, वैसे वह हिलती है, लेकिन वह न धागे को देख सकता है, न उसे, जो उसे हिलाता है…
वह उठ खड़ा हुआ। लड़की ने आतंकित हो कर उसे देखा, ‘आप कहाँ जा रहे हैं?’
‘वह नीचे नहीं आएँगी?’ उसने पूछा।
‘उन्हें मालूम है, आप यहाँ हैं।’ लड़की ने कुछ खीज कर कहा।
‘इसीलिए वह नहीं आना चाहतीं?’
‘नहीं…।’ लड़की ने कहा, ‘इसीलिए वह कभी भी आ सकती हैं।’
कैसे पागल हैं! इतनी छोटी-सी बात नहीं समझ सकते। ‘आप बैठिए, मैं अभी इन सब चीजों को समेट लेती हूँ।’
वह फर्श पर उकड़ूँ बैठ गई; बड़ी सफाई से हर चीज को उठा कर कोने में रखने लगी। मखमल की जूती, पशमीने की शॉल, गुजरात एंपोरियम का बेडकवर। उसकी पीठ पिता की ओर थी, किंतु वह उसके हाथ देख सकता था, पतले और साँवले, बिल्कुल अपनी माँ की तरह, वैसे ही निस्संग और ठंडे, जो उसकी लाई चीजों को आत्मीयता से पकड़ते नहीं थे, सिर्फ अनमने भाव से अलग ठेल देते थे। वे एक ऐसी बच्ची के हाथ थे, जिसने सिर्फ माँ के सीमित और सुरक्षित स्नेह को छूना सीखा था, मर्द के उत्सुक और पीड़ित उन्माद को नहीं जो पिता के सेक्स की काली कंदरा से उमड़ता हुआ बाहर आता है।
अचानक लड़की के हाथ ठिठक गए। उसे लगा, कोई दरवाजे की घंटी बजा रहा है लेकिन दूसरे ही क्षण फोन का ध्यान आया जो जीने के नीचे कोटर में था और जंजीर से बँधे पिल्ले की तरह जोर-जोर से चीख रहा था। लड़की ने चीजें वैसे ही छोड़ दीं और लपकते हुए सीढ़ियों के पास गई, फोन उठाया, एक क्षण तक कुछ सुनाई नहीं दिया। फिर वह चिल्लाई –
‘मामा, आपका फोन!’
बच्ची बेनिस्टर के सहारे खड़ी थी, हाथ में फोन झुलाती हुई। ऊपर का दरवाजा खुला और जीना हिलने लगा। कोई नीचे आ रहा था, फिर एक सिर लड़की के चेहरे पर झुका, गुँथा हुआ जूड़ा और फोन के बीच एक पूरा चेहरा उभर आया…
‘किसका है?’ औरत ने अपने लटकते हुए जूड़े को पीछे धकेल दिया और लड़की के हाथ से फोन खींच लिया। आदमी कुर्सी से उठा… लड़की ने उसकी ओर देखा। ‘हलो,’ औरत ने कहा। ‘हलो, हलो,’ औरत की आवाज ऊपर उठी और तब उसे पता चला, कि यह उस स्त्री की आवाज है, जो उसकी पत्नी थी; वह उसे बरसों बाद भी सैकड़ों आवाजों की भीड़ में पहचान सकता था… ऊँची पिच पर हल्के-से काँपती हुई, हमेशा से सख्त, आहत, परेशान, उसकी देह की एकमात्र चीज, जो देह से परे आदमी की आत्मा पर खून की खरोंच खींच जाती थी… वह जैसे उठा था, वैसे ही बैठ गया।
लड़की मुस्करा रही थी।
वह हैंगर के आईने से आदमी का चेहरा देख रही थी – और वह चेहरा कुछ वैसा ही बेडौल दिखाई दे रहा था जैसे उम्र के आईने से औरत की आवाज – उल्टा, टेढ़ा, पहेली-सा रहस्यमय! वे तीनों व्यक्ति अनजाने में चार में बँट गए थे – लड़की, उसकी माँ, वह और उसकी पत्नी… घर जब गृहस्थी में बदलता है, तो अपने-आप फैलता जाता है…
‘तुम जेनी से बात करोगी?’ औरत ने लड़की से कहा और बच्ची जैसे इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी। वह उछल कर ऊपरी सीढ़ी पर आई और माँ से टेलीफोन ले लिया, ‘हलो जेनी, इट इज मी!’
वह दो सीढ़ियाँ नीचे उतरी; अब आदमी उसे पूरा-का-पूरा देख सकता था।
‘बैठो…’ आदमी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसके स्वर में एक बेबस-सा अनुनय था, मानो उसे डर हो कि कहीं उसे देख कर वह उल्टे पाँव न लौट जाए।
वह एक क्षण अनिश्चय में खड़ी रही। अब वापस मुड़ना निरर्थक था, लेकिन इस तरह उसके सामने खड़े रहने का भी कोई तुक नहीं था। वह स्टूल खींच कर टी.वी. के आगे बैठ गई।
‘कब आए?’ उसका स्वर इतना धीमा था कि आदमी को लगा, टेलीफोन पर कोई दूसरी औरत बोल रही थी।
‘काफी देर हो गई… मुझे तो पता भी न था कि तुम ऊपर के कमरे में हो!’
स्त्री चुपचाप उसे देखती रही।
आदमी ने जेब से रूमाल निकाला, पसीना पोंछा, मुस्कराने की कोशिश में मुस्कराने लगा। ‘मैं बहुत देर तक बाहर खड़ा रहा, मुझे पता नहीं था, घंटी खराब है। गैरेज खाली पड़ा था, मैंने सोचा, तुम दोनों कहीं बाहर गए हो… तुम्हारी कार?’ उसे मालूम था, फिर भी उसने पूछा।
‘सर्विसिंग के लिए गई है!’ स्त्री ने कहा। वह हमेशा से उसकी छोटी, बेकार की बातों से नफरत करती आई थी, जबकि आदमी के लिए वे कुछ ऐसे तिनके थे, जिन्हें पकड़ कर डूबने से बचा जा सकता था। कम-से-कम कुछ देर के लिए…
‘तुम्हें मेरा टेलीग्राम मिल गया था? मैं फ्रेंकफर्ट आया था, उसी टिकट पर यहाँ आ गया; कुछ पौंड ज्यादा देने पड़े। मैंने तुम्हें वहाँ से फोन भी किया, लेकिन तुम दोनों कहीं बाहर थे…’
‘कब?’ औरत ने हल्की जिज्ञासा से उसकी ओर देखा, ‘हम दोनों घर में थे।’
‘घंटी बज रही थी, लेकिन किसी ने उठाया नहीं। हो सकता है, आपरेटर मेरी अंग्रेजी नहीं समझ सकी और गलत नंबर दे दिया हो! लेकिन सुनो।’ वह हँसने लगा, ‘एक अजीब बात हुई। हीथ्रो पर मुझे एक औरत मिली, जो पीछे से बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखाई दे रही थी, यह तो अच्छा हुआ, मैंने उसे बुलाया नहीं… हिंदुस्तान के बाहर हिंदुस्तानी औरतें एक जैसी ही दिखाई देती हैं…।’ वह बोले जा रहा था। वह उस आदमी की तरह था जो आँखों पर पट्टी बाँध कर हवा में तनी हुई रस्सी पर चलता है, स्त्री कहीं बहुत नीचे थी, एक सपने में, जिसे वह बहुत पहले कभी जानता था, किंतु अब उसे याद नहीं आ रहा था कि वह उसके सामने क्यों बैठा था?
वह चुप हो गया। उसे खयाल आया, इतनी देर से वह सिर्फ अपनी आवाज सुन रहा है, उसके सामने बैठी स्त्री बिल्कुल चुप बैठी थी। उसकी ओर बहुत ठंडी और हताश निगाहों से देख रही थी।
‘क्या बात है?’ आदमी ने कुछ भयभीत-सा हो कर पूछा।
‘मैंने तुमसे मना किया था; तुम समझते क्यों नहीं?’
‘किसके लिए? तुमने किसके लिए मना किया था?’
‘मैं तुमसे कुछ नहीं चाहती… मेरे घर तुम ये सब क्यों लाते हो? क्या फायदा है इनका?’
पहले क्षण वह नहीं समझा, कौन-सी चीजें? फिर उसकी निगाहें फर्श पर गईं… शांति-निकेतन का पर्स, डाक टिकटों का अल्बम, दालबीजी का डिब्बा – वे अब बिल्कुल लुटी-पिटी दिखाई दे रही थीं, जैसे वह कुर्सी पर बैठा हुआ था, वैसी वे फर्श पर बिखरी हुई। ‘कौन-सी ज्यादा हैं?’ उसने खिसियाते हुए कहा, ‘इन्हें न लाता तो आधा सूटकेस खाली पड़ा रहता।’
‘लेकिन मैं तुमसे कुछ नहीं चाहती… तुम क्या इतनी-सी बात नहीं समझ सकते?’
स्त्री की आवाज काँपती हुई ऊपर उठी, जिसके पीछे न जाने कितनी लड़ाइयों की पीड़ा, कितने नरकों का पानी भरा था, जो बाँध टूटते ही उसके पास आने लगा, एक-एक इंच आगे बढ़ता हुआ। उसने जेब से रूमाल निकाला और अपने लथपथ चेहरे को पोंछने लगा।
‘क्या तुम्हें इतनी देर के लिए आना भी बुरा लगता है?’
‘हाँ…।’ उसका चेहरा तन गया, फिर अजीब हताशा में वह ढीली पड़ गई, ‘मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती – बस!’
क्या यह इतना आसान है? वह जिद्दी लड़के की तरह उसे देखने लगा, जो सवाल समझ लेने के बाद भी बहाना करता है कि उसे कुछ समझ में नहीं आया।
‘वुक्कू!’ उसने धीरे से कहा, ‘प्लीज!’
‘मुझे माफ करो…।’ औरत ने कहा।
‘तुम चाहती क्या हो?’
‘लीव मी अलोन…। इससे ज्यादा मैं कुछ और नहीं चाहती।’
‘मैं बच्ची से भी मिलने नहीं आ सकता?’
‘इस घर में नहीं, तुम उससे कहीं बाहर मिल सकते हो?’
‘बाहर!’ आदमी ने हकबका कर सिर उठाया, ‘बाहर कहाँ?’
उस क्षण वह भूल गया कि बाहर सारी दुनिया फैली है, पार्क, सड़कें, होटल के कमरे – उसका अपना संसार – बच्ची कहाँ-कहाँ उसके साथ घिसटेगी?
वह फोन पर हँस रही थी। कुछ कह रही थी, ‘नहीं, आज मैं नहीं आ सकती। डैडी घर में हैं, अभी-अभी आ रहे हैं… नहीं, मुझे मालूम नहीं। मैंने पूछा नहीं…।’ क्या नहीं मालूम? शायद उसकी सहेली ने पूछा था, वह कितने दिन रहेगा? सामने बैठी स्त्री भी शायद यह जानना चाहती थी, कितना समय, कितनी घड़ियाँ, कितनी यातना अभी और उसके साथ भोगनी पड़ेगी?
शाम की आखिरी धूप भीतर आ रही थी। टी.वी. का स्क्रीन चमक रहा था, लेकिन वह खाली था और उसमें सिर्फ स्त्री की छाया बैठी थी, जैसे खबरें शुरू होने से पहले एनांउसर की छवि दिखाई देती है, पहले कमजोर और धुँधली, फिर धीरे-धीरे ‘ब्राइट’ होती हुई… वह साँस रोके प्रतीक्षा कर रहा था कि वह कुछ कहेगी हालाँकि उसे मालूम था कि पिछले वर्षों से सिर्फ एक न्यूज-रील है जो हर बार मिलने पर एक पुरानी पीड़ा का टेप खोलने लगती है, जिसका संबंध किसी दूसरी जिंदगी से है… चीजें और आदमी कितनी अलग हैं! बरसों बाद भी घर, किताबें, कमरे वैसे ही रहते हैं, जैसा तुम छोड़ गए थे; लेकिन लोग? वे उसी दिन से मरने लगते हैं, जिस दिन से अलग हो जाते हैं… मरते नहीं, एक दूसरी जिंदगी जीने लगते हैं, जो धीरे-धीरे उस जिंदगी का गला घोंट देती है, जो तुमने साथ गुजारी थी…
‘मैं सिर्फ बच्ची से नहीं…’ वह हकलाने लगा, ‘मैं तुमसे भी मिलने आया था।’
‘मुझसे?’ औरत के चेहरे पर हँसी, हिकारत, हैरानी एक साथ उमड़ आईं, ‘तुम्हारी झूठ की आदत अभी तक नहीं गई!’
‘तुमसे झूठ बोल कर अब मुझे क्या मिलेगा?’
‘मालूम नहीं, तुम्हें क्या मिलेगा – मुझे जो मिला है, उसे मैं भोग रही हूँ।’ उसने एक ठहरी ठंडी निगाह से बाहर देखा। ‘मुझे अगर तुम्हारे बारे में पहले से ही कुछ मालूम होता, तो मैं कुछ कर सकती थी।’
‘क्या कर सकती थीं?’ एक ठंडी-सी झुरझुरी ने आदमी को पकड़ लिया।
‘कुछ भी। मैं तुम्हारी तरह अकेली नहीं रह सकती; लेकिन अब इस उम्र में… अब कोई मुझे देखता भी नहीं।’
‘वुक्कू…!’ उसने हाथ पकड़ लिया।
‘मेरा नाम मत लो… वह सब खत्म हो गया।’
वह रो रही थी; बिल्कुल निस्संग, जिसका गुजरे हुए आदमी और आनेवाली उम्मीद – दोनों से कोई सरोकार नहीं थी। आँसू, जो एक कारण से नहीं, पूरा पत्थर हट जाने से आते हैं, एक ढलुआ जिंदगी पर नाले की तरह बहते हुए; औरत बार-बार उन्हें अपने हाथ से झटक देती थी…
बच्ची कब से फोन के पास चुप बैठी थी। वह जीने की सबसे निचली सीढ़ी पर बैठी थी और सूखी आँखों से रोती माँ को देख रही थी। उसके सब प्रयत्न निष्फल हो गए थे, किंतु उसके चेहरे पर निराशा नहीं थी। हर परिवार के अपने दुःस्वप्न होते हैं, जो एक अनवरत पहिए में घूमते हैं; वह उसमें हाथ नहीं डालती थी। इतनी कम उम्र में वह इतना बड़ा सत्य जान गई थी कि मनुष्य के मन और बाहर की सृष्टि में एक अद्भुत समानता है – वे जब तक अपना चक्कर पूरा नहीं कर लेते, उन्हें बीच में रोकना बेमानी है…।
वह बिना आदमी को देखे माँ के पास गई; कुछ कहा, जो उसके लिए नहीं था। औरत ने उसे अपने पास बैठा लिया, बिल्कुल अपने से सटा कर। काउच पर बैठी वे दोनों दो बहनों-सी लग रही थीं। वे उसे भूल गई थीं। कुछ देर पहले जो ज्वार उठा था, उसमें घर डूब गया था लेकिन अब पानी वापस लौट गया था और अब आदमी वहाँ था, जहाँ उसे होना चाहिए था – किनारे पर। उसे यह ईश्वर का वरदान जैसा जान पड़ा; वह दोनों के बीच बैठा है – अदृश्य! बरसों से उसकी यह साध रही थी कि वह माँ और बेटी के बीच अदृश्य बैठा रहे। सिर्फ ईश्वर ही अपनी दया में अदृश्य होता है – यह उसे मालूम था। किंतु जो आदमी गढ़हे की सबसे निचली सतह पर जीता है, उसे भी कोई नहीं देख सकता। माँ और बच्ची ने उसे अलग छोड़ दिया था; यह उसकी उपेक्षा नहीं थी। उसकी तरफ से मुँह मोड़ कर उन्होंने उसे अपने पर छोड़ दिया था – ठीक वहीं – जहाँ उसने बरसों पहले घर छोड़ा था।
लड़की माँ को छोड़ कर उसके पास आ कर बैठ गई।
‘हमारा बाग देखने चलोगे?’ उसने कहा।
‘अभी?’ उसने कुछ विस्मय से लड़की को देखा। वह कुछ अधीर और उतावली-सी दिखाई दे रही थी, जैसे वह उससे कुछ कहना चाहती हो, जिसे कमरे के भीतर कहना असंभव हो।
‘चलो,’ आदमी ने उठते हुए कहा, ‘लेकिन पहले इन चीजों को ऊपर ले जाओ।’
‘हम इन्हें बाद में समेट लेंगे।’
‘बाद में कब?’ आदमी ने कुछ सशंकित हो कर पूछा।
‘आप चलिए तो!’ लड़की ने लगभग उसे घसीटते हुए कहा।
‘इनसे कहो, अपना सामान सूटकेस में रख लें।’ स्त्री की आवाज सुनाई दी।
उसे लगा, किसी ने अचानक पीछे से धक्का दिया हो। वह चमक कर पीछे मुड़ा, ‘क्यों?’
‘मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं है।’
उसके भीतर एक लपलपाता अंधड़ उठने लगा, ‘मैं नहीं ले जाऊँगा, तुम चाहो तो इन्हें बाहर फेंक सकती हो।’
‘बाहर?’ स्त्री की आवाज थरथरा रही थी, ‘मैं इनके साथ तुम्हें भी बाहर फेंक सकती हूँ।’ रोने के बाद उसकी आँखें चमक रही थीं; गालों का गीलापन सूखे काँच-सा जम गया था, जो पोंछे हुए नहीं, सूखे हुए आँसुओं से उभर कर आता है।
‘क्या हम बाग देखने नहीं चलेंगे?’ बच्ची ने उसका हाथ खींचा – और वह उसके साथ चलने लगा। वह कुछ भी नहीं देख रहा था। घास, क्यारियाँ और पेड़ एक गूँगी फिल्म की तरह चल रहे थे। सिर्फ उसकी पत्नी की आवाज एक भुतैली कमेंट्री की तरह गूँज रही थी – बाहर, बाहर!
‘आप ममी के साथ बहस क्यों करते हैं?’ लड़की ने कहा।
‘मैंने बहस कहाँ की?’ उसने बच्ची को देखा – जैसे वह भी उसकी दुश्मन हो।
‘आप करते हैं।’ लड़की का स्वर अजीब-सा हठीला हो आया था। वह अंग्रेजी में ‘यू’ कहती थी, जिसका मतलब प्यार में ‘तुम’ होता था और नाराजगी में ‘आप’। अंग्रेजी सर्वनाम की यह संदिग्धता बाप-बेटी के रिश्ते को हवा में टाँगे रहती थी, कभी बहुत पास, कभी बहुत पराया – जिसका सही अंदाज उसे सिर्फ लड़की की टोन में टटोलना पड़ता था। एक अजीब-से भय ने आदमी को पकड़ लिया। वह एक ही समय में माँ और बच्ची दोनों को नहीं खोना चाहता था।
‘बड़ा प्यारा बाग है,’ उसने फुसलाते हुए कहा, ‘क्या माली आता है?’
‘नहीं, माली नहीं।’ लड़की ने उत्साह से कहा, ‘मैं शाम को पानी देती हूँ और छुट्टी के दिन ममी घास काटती हैं… इधर आओ, मैं तुम्हें एक चीज दिखाती हूँ।’
वह उसके पीछे-पीछे चलने लगा। लॉन बहुत छोटा था – हरा, पीला, मखमली। पीछे गैराज था और दोनों तरफ झाड़ियों की फेंस लगी थी। बीच में एक घना, बूढ़ा, विलो खड़ा था। लड़की पेड़ के पीछे छिप-सी गई, फिर उसकी आवाज सुनाई दी, ‘कहाँ हो तुम?’
वह चुपचाप, दबे-पाँवों से पेड़ के पीछे चला आया और हैरान-सा खड़ा रहा। विलो और फेंस के बीच काली लकड़ी का बाड़ा था, जिसके दरवाजे से एक खरगोश बाहर झाँक रहा था; दूसरा खरगोश लड़की की गोद में था। वह उसे ऐसे सहला रही थी, जैसे वह ऊन का गोला हो, जो कभी भी हाथ से छूट कर झाड़ियों में गुम हो जाएगा।
‘ये हमने अभी पाले हैं… पहले दो थे, अब चार।’
‘बाकी कहाँ हैं?’
‘बाड़े के भीतर… वे अभी बहुत छोटे हैं।’
पहले उसका मन भी खरगोश को छूने के लिए हुआ, किंतु उसका हाथ अपने-आप बच्ची के सिर पर चला गया और वह धीरे-धीरे उसके भूरे, छोटे बालों से खेलने लगा। लड़की चुप खड़ी रही और खरगोश अपनी नाक सिकोड़ता हुआ उसकी ओर ताक रहा था।
‘पापा?’ लड़की ने बिना सिर उठाए धीरे से कहा, ‘क्या आपने डे-रिटर्न का टिकट लिया है?’
‘नहीं; क्यों?’
‘ऐसे ही; यहाँ वापसी का टिकट बहुत सस्ता मिल जाता है।’
क्या उसने यही पूछने के लिए उसे यहाँ बुलाया था? उसने धीरे से अपना हाथ लड़की के सिर से हटा लिया।
‘आप रात को कहाँ रहेंगे?’ लड़की का स्वर बिल्कुल भावहीन था।
‘अगर मैं यहीं रहूँ तो?’
लड़की ने धीरे से खरगोश को बाड़े में रख दिया और खट से दरवाजा बंद कर दिया।
‘मैं हँसी कर रहा था,’ उसने हँस कर कहा, ‘मैं आखिरी ट्रेन से लौट जाऊँगा।’
लड़की ने मुड़ कर उसकी ओर देखा, ‘यहाँ दो-तीन अच्छे होटल भी हैं…। मैं अभी फोन करके पूछ लेती हूँ।’ बच्ची का स्वर बहुत कोमल हो आया। यह जानते ही कि वह रात को घर में नहीं ठहरेगा, वह माँ से हट कर आदमी के साथ हो गई; धीरे से उसका हाथ पकड़ा, उसे वैसे ही सहलाने लगी, जैसे अभी कुछ देर पहले खरगोश को सहला रही थी। लेकिन आदमी का हाथ पसीने से तरबतर था।
‘सुनो, मैं अगली छुट्टियों में इंडिया आऊँगी – इस बार पक्का है।’
उसे कुछ आश्चर्य हुआ कि आदमी ने कुछ नहीं कहा; सिर्फ बाड़े में खरगोशों की खटर-पटर सुनाई दे रही थी।
‘पापा… तुम कुछ बोलते क्यों नहीं?’
‘तुम हर साल यही कहती हो।’
‘कहती हूँ… लेकिन इस बार मैं आऊँगी, डोंट यू बिलीव मी?… भीतर चलें? ममी हैरान हो रही होंगी कि हम कहाँ रह गए।’
अगस्त का अँधेरा चुपचाप चला आया था। हवा में विलो की पत्तियाँ सरसरा रही थीं। कमरों के परदे गिरा दिए गए थे, लेकिन रसोई का दरवाजा खुला था। लड़की भागते हुए भीतर गई और सिंक का नल खोल कर हाथ धोने लगी। वह उसके पीछे आ कर खड़ा हो गया; सिंक के ऊपर आईने में उसने अपना चेहरा देखा – रूखी गर्द और बढ़ी हुई दाढ़ी और सुर्ख आँखों के बीच उसकी ओर हैरत में ताकता हुआ – नहीं, तुम्हारे लिए कोई उम्मीद नहीं…
पापा, क्या तुम अब भी अपने-आपसे बोलते हो?’ लड़की ने पानी में भीगा अपना चेहरा उठाया – वह शीशे में उसे देख रही थी।
‘हाँ, लेकिन अब मुझे कोई सुनता नहीं…।’ उसने धीरे से बच्ची के कंधे पर हाथ रखा, ‘क्या फ्रिज में सोडा होगा?’
‘तुम भीतर चलो, मैं अभी लाती हूँ।’
कमरे में कोई न था। उसकी चीजें बटोर दी गई थीं। सूटकेस कोने में खड़ा था; जब वे बाग में थे, उसकी पत्नी ने शायद उन सब चीजों को देखा होगा; उन्हें छुआ होगा। वह उससे चाहे कितनी नाराज क्यों न हो – चीजों की बात अलग थी। वह उन्हें ऊपर नहीं ले गई थी, लेकिन दुबारा सूटकेस में डालने की हिम्मत नहीं की थी… उसने उन्हें अपने भाग्य पर छोड़ दिया था।
कुछ देर बाद जब बच्ची सोडा और गिलास ले कर आई, तो उसे सहसा पता नहीं चला कि वह कहाँ बैठा है। कमरे में अँधेरा था – पूरा अँधेरा नहीं – सिर्फ इतना, जिसमें कमरे में बैठा आदमी चीजों के बीच चीज-जैसा दिखाई देता है, ‘पापा… तुमने बत्ती नहीं जलाई?’
‘अभी जलाता हूँ…।’ वह उठा और स्विच को ढूँढ़ने लगा, बच्ची ने सोडा और गिलास मेज पर रख दिया और टेबुल लैंप जला दिया।
‘ममी कहाँ हैं?’
‘वह नहा रही हैं, अभी आती होंगी।’
उसने अपने बैग से व्हिस्की निकाली, जो उसने फ्रेंकफर्ट के एयरपोर्ट पर खरीदी थी… गिलास में डालते हुए उसके हाथ ठिठक गए, ‘तुम्हारी जिंजर-एल कहाँ है?’
‘मैं अब असली बियर पीती हूँ।’ लड़की ने हँस कर उसकी ओर देखा, ‘तुम्हें बर्फ चाहिए?’
‘नहीं… लेकिन तुम जा कहाँ रही हो?’
‘बाड़े में खाना डालने… नहीं तो वे एक-दूसरे को मार खाएँगे।’
वह बाहर गई तो खुले दरवाजे से बाग का अँधेरा दिखाई दिया – तारों की पीली तलछट में झिलमिलाता हुआ। हवा नहीं था। बाहर का सन्नाटा घर की अदृश्य आवाजों के भीतर से छन कर आता था। उसे लगा, वह अपने घर में बैठा है और जो कभी बरसों पहले होता था, वह अब हो रहा है। वह शॉवर के नीचे गुनगुनाती रहती थी और जब वह बालों पर तौलिया साफे की तरह बाँध कर बाहर निकलती थी, तब पानी की बूँदें बाथरूम से ले कर उसके कमरे तक एक लकीर बनाती जाती थीं – पता नहीं वह लकीर कहाँ बीच में सूख गई? कौन-सी जगह, किस खास मोड़ पर वह चीज हाथ से छूट गई, जिसे वह कभी दोबारा नहीं पकड़ सका?
उसने कुछ और व्हिस्की डाली; हालाँकि गिलास अभी खाली नहीं हुआ था। उसे कुछ अजीब लगा कि पिछली रात भी यही घड़ी थी जब वह पी रहा था, लेकिन तब वह हवा में था। जब उसे एयर-होस्टेज की आवाज सुनाई दी कि हम चैनल पार कर रहे हैं तो उसने हवाई जहाज की खिड़की से नीचे देखा – कुछ भी दिखाई नहीं देता था – न समुद्र, न लाइटहाउस, सिर्फ अँधेरा, अँधेरे में बहता हुआ अँधेरा – फिर कुछ भी नहीं। और तब नीचे अँधेरे में झाँकते हुए उसे खयाल आया कि वह चैनल जो नीचे कहीं दिखाई नहीं देता था, असल में कहीं भीतर है – उसकी एक जिंदगी से दूसरी जिंदगी तक फैला हुआ; जिसे वह हमेशा पार करता रहेगा, कभी इधर, कभी उधर, कहीं का भी नहीं, न कहीं से आता हुआ, न कहीं पहुँचता हुआ…।
‘बिंदु कहाँ है?’ उसने चौंक कर ऊपर देखा, वह वहाँ कब से खड़ी थी, उसे पता नहीं चला था। ‘बाहर बाग में,’ उसने कहा, ‘खरगोशों को खाना देने।’
वह अलग खड़ी थी, बेनिस्टर के नीचे। नहाने के बाद उसने एक लंबी मैक्सी पहन ली थी…। बाल खुले थे। चेहरा बहुत धुला और चमकीला-सा लग रहा था। वह मेज पर रखे उसके गिलास को देख रही थी। उसका चेहरा शांत था; शॉवर ने जैसे न केवल उसके चेहरे को, बल्कि उसके संताप को भी धो डाला था।
‘बर्फ भी रखी है।’ उसने कहा।
‘नहीं, मैंने सोडा ले लिया; तुम्हारे लिए एक बना दूँ?’
उसने सिर हिलाया, जिसका मतलब कुछ भी था, उसे मालूम था कि गर्म पानी से नहाने के बाद उसे कुछ ठंडा पीना अच्छा लगता था। अर्से बाद भी वह उसकी आदतें नहीं भूला था, बल्कि उन आदतों के सहारे ही दोनों के बीच पुरानी पहचान लौट आती थी। वह रसोई में गया और उसके लिए एक गिलास ले आया। उसमें थोड़ी-सी बर्फ डाली। जब व्हिस्की मिलाने लगा, तो उसकी आवाज सुनाई दी, ‘बस, इतनी काफी है।’
वह धुली हुई आवाज थी, जिसमें कोई रंग नहीं था, न स्नेह का, न नाराजगी का – एक शांत और तटस्थ आवाज। वह सीढ़ियों से हट कर कुर्सी के पास चली आई थी।
‘तुम बैठोगी नहीं?’ उसने कुछ चिंतित हो कर पूछा।
उसने अपना गिलास उठाया और वहीं स्टूल पर बैठ गई, जहाँ दुपहर को बैठी थी। टी.वी. के पास लेकिन टेबुल-लैंप से दूर – जहाँ सिर्फ रोशनी की एक पतली-सी झाँई, उस तक पहुँच रही थी।
कुछ देर तक दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला, फिर स्त्री की आवाज सुनाई दी, ‘घर में सब लोग कैसे हैं?’
‘ठीक हैं… ये सब चीजें उन्होंने ही भेजी हैं।’
‘मुझे मालूम है,’ औरत ने कुछ थके स्वर में कहा, ‘क्यों उन बेचारों को तंग करते हो? तुम ढो-ढो कर इन चीजों को लाते हो और वे यहाँ बेकार पड़ी रहती हैं।’
‘वे यही कर सकते हैं,’ उसने कहा, ‘तुम बरसों से वहाँ गई नहीं; वे बहुत याद करते हैं।’
‘अब जाने का कोई फायदा है?’ उसने गिलास से लंबा घूँट लिया, ‘मेरा अब उनसे कोई रिश्ता नहीं।’
‘तुम बच्ची के साथ तो आ सकती हो, उसने अभी तक हिंदुस्तान नहीं देखा।’
वह कुछ देर चुप रही… फिर धीरे से कहा, ‘अगले साल वह चौदह वर्ष की हो जाएगी… कानून के मुताबिक तब वह कहीं भी जा सकती है।’
‘मैं कानून की बात नहीं कर रहा; तुम्हारे बिना वह कहीं नहीं जाएगी।’
स्त्री ने गिलास की भीगी सतह से आदमी को देखा, ‘मेरा बस चले तो उसे वहाँ कभी न भेजूँ।’
‘क्यों?’ आदमी ने उसकी ओर देखा।
वह धीरे से हँसी, ‘क्या हम दो हिंदुस्तानी उसके लिए काफी नहीं हैं?’
वह बैठा रहा। कुछ देर बाद रसोई का दरवाजा खुला, लड़की भीतर आई, चुपचाप दोनों को देखा और फिर जीने के पास चली गई जहाँ टेलीफोन रखा था।
‘किसे कर रही हो?’ औरत ने पूछा।
लड़की चुप रही, फोन का डायल घुमाने लगी।
आदमी उठा, उसकी ओर देखा, ‘थोड़ा-सा और लोगी?’
‘नहीं…।’ उसने सिर हिलाया। आदमी धीरे-धीरे अपने गिलास में डालने लगा।
‘क्या बहुत पीने लगे हो?’ औरत ने कहा।
‘नहीं…।’ आदमी ने सिर हिलाया, ‘सफर में कुछ ज्यादा ही हो जाता है।’
‘मैंने सोचा था, अब तक तुमने घर बसा लिया होगा।’
‘कैसे?’ उसने स्त्री को देखा, ‘तुम्हें यह कैसे भ्रम हुआ?’
औरत कुछ देर तक नीरव आँखों से उसे देखती रही, ‘क्यों, उस लड़की का क्या हुआ? वह तुम्हारे साथ नहीं रहती?’ स्त्री के स्वर में कोई उत्तेजना नहीं थी, न क्लेश की कोई छाया थी… जैसे दो व्यक्ति मुद्दत बाद किसी ऐसी घटना की चर्चा कर रहे हों जिसने एक झटके से दोनों को अलग छोरों पर फेंक दिया था।
‘मैं अकेला रहता हूँ… माँ के साथ।’ उसने कहा।
औरत ने तनिक विस्मय से उसे देखा, ‘क्या बात हुई?’
‘कुछ नहीं… मैं शायद साथ रहने के काबिल नहीं हूँ।’ उसका स्वर असाधारण रूप से धीमा हो आया, जैसे वह उसे अपनी किसी गुप्त बीमारी के बारे में बता रहा हो, ‘तुम हैरान हो? लेकिन ऐसे लोग होते हैं…’ वह कुछ और कहना चाहता था, प्रेम के बारे में, वफादारी के बारे में, विश्वास और धोखे के बारे में; कोई बड़ा सत्य, जो बहुत-से झूठों से मिल कर बनता है, व्हिस्की की धुंध में बिजली की तरह कौंधता है और दूसरे क्षण हमेशा के लिए अँधेरे में लोप हो जाता है…
लड़की शायद इस क्षण की ही प्रतीक्षा कर रही थी; वह टेलीफोन से उठ कर आदमी के पास आई, एक बार माँ को देखा, वह टेबुल-लैंप के पीछे अँधेरे के आधे कोने में छिप गई थीं, और आदमी? वह गिलास के पीछे सिर्फ एक डबडबाता-सा धब्बा बन कर रह गया था।
‘पापा,’ लड़की के हाथ में कागज का पुरजा था, ‘यह होटल का नाम है, टैक्सी तुम्हें सिर्फ दस मिनट में पहुँचा देगी।’
उसने लड़की को अपने पास खींच लिया और कागज जेब में रख लिया। कुछ देर तक तीनों चुप बैठे रहे, जैसे बरसों पहले यात्रा पर निकलने से पहले घर के सब प्राणी एक साथ सिमट कर चुप बैठ जाते थे। बाहर बहुत-से तारे निकल आए थे, जिसमें बूढ़ी, विलो, झाड़ियाँ और खरगोशों का बाड़ा एक निस्पंद पीले आलोक में पास-पास सरक आए थे।
उसने अपना गिलास मेज पर रखा, फिर धीरे से लड़की को चूमा, अपना सूटकेस उठाया और जब लड़की ने दरवाजा खोला, तो वह क्षण भर देहरी पर ठिठक गया, ‘मैं चलता हूँ।’ उसने कहा। पता नहीं, यह बात उसने किससे कही थी, किंतु जहाँ वह बैठी थी, वहाँ से कोई आवाज नहीं आई। वहाँ उतनी ही घनी चुप्पी थी, जितनी बाहर अँधेरे में, जहाँ वह जा रहा था।
=========================