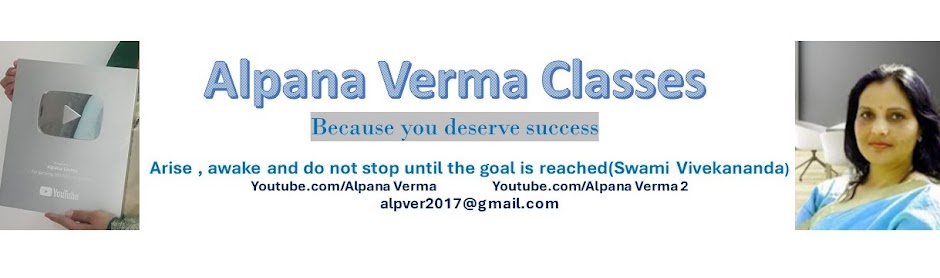Click on the title
- Home
- Soul food
- Treasure अमूल्य निधि
- Love connection स्नेह - अमृत
- Abhivyakti Madhyam NCERT
- 🥇✔Hindi Grammar हिंदी व्याकरण
- |Class 9 Sparsh/Sanchayan|
- |Class 10 Sparsh/Sanchayan|
- |Class 9 Kshitij /Kritika|
- |Class 10 Kshitij Kritika|
- |Class 11 Aaroh/ Vitan|
- |Class 12 Aaroh/Vitan|
- |Class 11 Antra/Antral|
- |Class 12 Antra/Antral|
- |Essay /Paragraph |
- ICSE 9 &10 Hindi|
- |Hindi Writers- Poets |
- |UP Board Class 10|
- |Bihar Board Class 12|
- |UGC/NET/JRF Hindi 2021 |
- |RPSC Grade 1 & 2 Teacher Hindi|
- ISC हिन्दी 11& 12
- एक दुनिया समानांतर
Wednesday, July 26, 2023
Friday, July 7, 2023
Thursday, July 6, 2023
सुभान खाँ /माटी की मूरतें /रामवृक्ष बेनीपुरी
औडियो सुनिए
सुभान खाँ
रामवृक्ष बेनीपुरी
क्या आपका अल्लाह पच्छिम में रहता है? वह पूरब क्यों नहीं रहता? 'सुभान दादा की लंबी, सफ़ेद, चमकती, रोब बरसाती दाढ़ी में अपनी नन्ही उँगलियों को घुमाते हुए मैंने पूछा। उनकी चौड़ी, उभरी पेशानी पर एक उल्लास की झलक और दाढ़ी-मूँछ की सघनता में दबे, पतले अधरों पर एक मुस्कान की रेखा दौड़ गई। अपनी लंबी बाँहों की दाहिनी हथेली मेरे सिर पर सहलाते हुए उन्होंने कहा—
नहीं बबुआ, अल्लाह तो पूरब पश्चिम, उत्तर दक्षिण सब ओर है।
तो फिर आप पश्चिम मुँह खड़े होकर ही नमाज़ क्यों पढ़ते हैं?
पश्चिम और के मुल्क में अल्लाह के रसूल आए थे जहाँ रसूल आए थे, वहाँ हमारे तीरथ हैं। उन्हीं तीरथों की ओर मुँह करके अल्लाह को याद करते हैं।
वे तीरथ यहाँ से कितनी दूर होंगे?
“बहुत दूरी
जहाँ सूरज देवता डूबते हैं?'
“नहीं, उससे कुछ इधर ही!
“आप उन तीरथों में गए हैं, सुभान दादा?
देखा, सुभान दादा की बड़ी-बड़ी आँखों में आँसू डबडबा आए। उनका चेहरा लाल हो उठा। भाव-विभोर हो गद्गद कंठ से बोले—
वहाँ जाने में बहुत ख़र्च पड़ते हैं, बबुआ! मैं ग़रीब आदमी ठहरा! इस बुढ़ापे में भी इतनी मेहनत मशक़्क़त कर रहा हूँ कि कहीं कुछ पैसे बचा पाऊँ और उस पाक जगह की ज़ियारत कर आऊँ!
उनकी आँखों को देखकर मेरा बचपन का दिल भी भावना से ओत-प्रोत हो गया। मैंने उनसे कहा, मेरे मामाजी से कुछ क़र्ज़ क्यों नहीं ले लेते, दादा?
क़र्ज़ के पैसे से तीरथ करने में सबाब नहीं मिलता, बबुआ! अल्लाह ने चाहा तो एक दो साल में इतने जमा हो जाएँगे कि किसी तरह वहाँ जा सकूँ।
वहाँ से मेरे लिए भी कुछ सौगात लाइएगा न? क्या लाइएगा?
वहाँ से लोग खजूर और छुहारे लाते हैं।
हाँ हाँ, मेरे लिए छुहारे ही लाइएगा; लेकिन एक दर्जन से कम नहीं लूँगा, हूँ।
सुभान दादा की सफ़ेद दाढ़ी-मूँछ के बीच उनके सफ़ेद दाँत चमक रहे थे। कुछ देर तक मुझे दुलारते रहे। फिर कुछ रुककर बोले, अच्छा जाइए, खेलिए, मैं ज़रा काम पूरा कर लूँ। मज़दूरी भर काम नहीं करने से अल्लाह नाराज़ हो जाएँगे।
क्या आपके अल्लाह बहुत गुस्सावर हैं? मैं तुनककर बोला।
आज सुभान दादा बड़े ज़ोरों से हँस पड़े, फिर एक बार मेरे सिर पर हथेली फेरी और बोले, बच्चों से वह बहुत ख़ुश रहते हैं, बबुआ! वह तुम्हारी उम्रदराज़ करें। कहकर मुझे अपने कंधे पर ले लिया। मुझे लेते हुए दीवार के नज़दीक आए वहाँ उतार दिया और झट अपनी कन्नी और बसूली से दीवार पर काम करने लगे।
सुभान ख़ाँ एक अच्छे राज समझे जाते थे। जब-जब घर की दीवारों पर कुछ मरम्मत की ज़रूरत होती है, उन्हें बुला लिया जाता है। आते हैं, पाँच-सात रोज़ यहीं रहते हैं, काम ख़त्म कर चले जाते हैं।
लंबा-चौड़ा, तगड़ा है बदन इनका पेशानी चौड़ी, भवें बड़ी सघन और उभरी आँखों के कोनों में कुछ लाली और पुतलियों में कुछ नीलेपन की झलक नाक असाधारण ढंग से नुकीली दाढ़ी सघन—इतनी लंबी कि छाती तक पहुँच जाए। वह छाती, जो बुढ़ापे में भी फैली फूली हुई। सिर पर हमेशा ही एक दुपलिया टोपी पहने होते और बदन में नीमस्तीन। कमर में कच्छे वाली धोती, पैर में चमरौंधा जूता। चेहरे से नूर टपकता, मुँह से शहद झरता। भलेमानसों के बोलने चालने, बैटने-उठने के क़ायदे की पूरी पाबंदी करते वह।
किंतु, बचपन में मुझे सबसे अधिक भाती उनकी वह सफ़ेद चमकती हुई दाढ़ी। नमाज़ के वक़्त कमर में धारीदार लुंगी और शरीर में सादा कुरता पहन, घुटने टेक, दोनों हाथ छाती से ज़रा ऊपर उठा, आधी आँखें मूँदकर जब वह कुछ मंत्र-सा पढ़ने लगते, मैं विस्मय-विमुग्ध होकर उन्हें देखता रह जाता! मुझे ऐसा मालूम होता—सचमुच उनके अल्लाह वहाँ आ गए हैं! दादा की झपकती आँखें उन्हें देख रही हैं और वे होंठों-होंठों की बातें उन्हीं से हो रही हैं।
एक दिन बचपन के आवेश में मैंने उनसे पूछ भी लिया, सुभान दादा, आपने कभी अल्लाह को देखा है? 'यह क्या कह रहे हो, बबुआ? इंसान इन आँखों से अल्लाह को देख नहीं सकता।
मुझे धोखा मत दीजिए, दादा! मैं सब देखता हूँ आप रोज़ आधी आँखों से उन्हें देखते हैं, उनसे बुदबुदा बातें करते हैं। हाँ हाँ, मुझे चकमा दे रहे हैं आप!
मैं उनसे बातें करूँगा, मेरी ऐसी तक़दीर कहाँ? सिर्फ़ रसूल की उनसे बातें होती थीं, बबुआ ये बातें कुरान में लिखी हैं।
“अच्छा दादा, क्या आपके रसूल को भी दाढ़ी थी?
हाँ-हाँ, थी। बड़ी ख़ूबसूरत, लंबी सुनहली अब भी उनकी दाढ़ी कुछ बाल मक्का में रखे हैं। हम अपने तीरथ में उन बालों के भी दर्शन करते हैं!
बड़ा होने पर जब दाढ़ी होगी, मैं भी दाढ़ी रखाऊँगा दादा ख़ूब लंबी दाढ़ी।
सुभान दादा ने मुझे उठाकर गोद में ले लिया, फिर कंधे पर चढ़कर इधर-उधर घुमाया। तरह-तरह की बातें सुनाई, कहानियाँ कहीं, मेरा मन बहलाकर कह फिर अपने काम में लग गए। मुझे मालूम होता था, काम और अल्लाह—ये ही दो चीज़ें संसार में उनके लिए सबसे प्यारी हैं। काम करते हुए अल्लाह को नहीं भूलते थे और अल्लाह से फुरसत पाकर फिर झट काम में जुट या जुत जाना पवित्र कर्तव्य समझते थे और काम और अल्लाह का यह सामंजस्य उनके दिल में प्रेम की वह मंदाकिनी बहाता रहता था, जिसमें मेरे जैसे बच्चे भी बड़े मज़े में डुबकियाँ लगा सकते थे, चुभकियाँ ले सकते थे।
नानी ने कहा, सवेरे नहा, खा लो आज तुम्हें हुसैन साहब के पैक में जाना होगा! सुभान ख़ाँ आते ही होंगे!
जिन कितने देवताओं की मनौती के बाद माँ ने मुझे प्राप्त किया था, उनमें एक हुसैन साहब भी थे। नौ साल की उम्र तक, जब तक जनेऊ नहीं हो गई थी, मुहर्रम के दिन मुसलमान बच्चों की तरह मुझे भी ताजिए के चारों और रंगीन छड़ी लेकर कूदना पड़ा है और गले में गंडे पहनने पड़े हैं। मुहर्रम उन दिनों मेरे लिए कितनी ख़ुशी का दिन था! नए कपड़े पहनता, उछलता कूदता, नए-नए चेहरे और तरह-तरह के खेल देखता, धूम-धक्कड़ में किस तरह चार पहर गुज़र जाते! इस मुहर्रम के पीछे जो रोमांचकारी हृदय को पिघलानेवाली, करुण रस से भरी दर्द-अंगेज़ घटना छिपी हैं, उन दिनों उसकी ख़बर भी कहाँ थी!
ख़ैर, मैं नहा धोकर, पहन ओढ़कर इंतिज़ार ही कर रहा था कि सुभान दादा पहुँच गए, मुझे कंधे पर ले लिया और अपने गाँव में ले गए।
उनका घर क्या था, बच्चों का अखाड़ा बना हुआ था। पोते-पोतियों, नाती नातिनों की भरमार थी उनके घर में। मेरी ही उम्र के बहुत बच्चे रंगीन कपड़ों से सजे-धजे—सब मानो मेरे ही इंतिज़ार में! जब पहुँचा, सुभान दादा की बूढ़ी बीवी ने मेरे गले में एक बद्धी डाल दी, कमर में घंटी बाँध दी, हाथ में दो लाल चूड़ियाँ दे दी और उन बच्चों के साथ मुझे लिए-दिए करबला की ओर चलीं। दिन भर उछला कुदा तमाशे देखे, मिठाइयाँ उड़ाई और शाम को फिर सुभान दादा के कंधे पर घर पहुँच गया।
ईंद-बक़रीद को न सुभान दादा हमें भूल सकते थे, न होली दीवाली को हम उन्हें! होली के दिन नानी अपने हाथों में पुए, खीर और गोश्त परोसकर सुभान दादा को खिलाती और तब मैं ही अपने हाथों से अबीर लेकर उनकी दाढ़ी में मलता एक बार जब उनकी दाढ़ी रंगीन बन गई थी, मुझे पुरानी बात याद आ गई। मैंने कहा—
सुभान दादा, रसूल की दाढ़ी भी तो ऐसी ही रंगीन रही होगी?
उस पर अल्लाह ने ही रंग दे रखा था, बबुआ! अल्लाह की उन पर ख़ास मेहरबानी थी। उनके जैसा नसीब हम मामूली इंसानों को कहाँ!
ऐसा कहकर झट आँखें मूँदकर कुछ बुदबुदाने लगे—जैसे वह ध्यान में उन्हें देख रहे हों!
मैं भी कुछ बड़ा हुआ, उधर दादा भी आख़िर हज कर ही आए। अब मैं बड़ा हो गया था, लेकिन उन्हें छुहारे की बात भूली नहीं थी। जब मैं छुट्टी में शहर के स्कूल से लौटा, दादा यह अनुपम सौगात लेकर पहुँचे। इधर उनके घर की हालत भी अच्छी हो चली थी। दादा के पुण्य और लायक़ बेटों की मेहनत ने काफ़ी पैसे इकट्ठे कर लिए थे लेकिन उनमें वही विनम्रता और सज्जनता थी और पहले की ही तरह शिष्टाचार निबाहा। फिर छुहारे निकाल मेरे हाथ पर रख दिए—“बबुआ, यह आपके लिए ख़ास अरब से लाया हूँ याद है न, आपने इसकी फ़रमाइश की थी। उनके नथुने आनंदातिरेक से हिल रहे थे।
छुहारे लिए सिर चढ़ाया—ख़्वाहिश हुई, आज फिर में बच्चा हो पाता और उनके कंधे से लिपटकर उनकी सफ़ेद दाढ़ी में, जो अब सचमुच नूरानी हो चली थी, उँगलियाँ घुसाकर उन्हें 'दादा, दादा' कहकर पुकार उठता! लेकिन न मैं अब बच्चा हो सकता था, न ज़बान में वह मासूमियत और पवित्रता रह गई थी! अँग्रेज़ी स्कूल के वातावरण ने अजीब अस्वाभाविकता हर बात में ला दी थी। पर हाँ, शायद एक ही चीज़ अब भी पवित्र रह गई थी—आँखों ने आँसू की छलकन से अपने को पवित्र कर चुपचाप ही उनके चरणों में श्रद्धांजलि चढ़ा दी।
हज से लौटने के बाद सुभान दादा का ज़ियादा वक़्त नमाज़-बंदगी में ही बीतता दिन भर उनके हाथों में तसबीह के दाने घूमते और उनकी ज़बान अल्लाह की रट लगाए रहती। अपने जवार भर में उनकी बुज़ुर्गी की धाक थीं। बड़े-बड़े झगड़ों की पंचायतों में दूर-दूर के हिंदू-मुसलमान उन्हें पंच मुक़र्रर करते, उनकी ईमानदारी और दयानतदारी की कुछ ऐसी ही धूम थी।
सुभान दादा का एक अरमान था—मस्जिद बनाने का। मेरे मामा का मंदिर उन्होंने ही बनाया था। उन दिनों वह साधारण राज थे लेकिन तो भी कहा करते—'अल्लाह ने चाहा तो मैं एक मस्जिद ज़रूर बनवाऊँगा।
अल्लाह ने चाहा और वैसा दिन आया। उनकी मस्जिद भी तैयार हुई। गाँव के ही लायक़ एक छोटी सी मस्जिद, लेकिन बड़ी ही ख़ूबसूरत दादा ने अपनी ज़िंदगी भर की अर्जित कला इसमें ख़र्च कर दी थी। हाथ में इतनी ताक़त नहीं रह गई थी कि अब ख़ुद कन्नी या बसूली पकड़ें, लेकिन दिन भर बैठे-बैठे एक-एक ईंट की जुड़ाई पर ध्यान रखते और उसके भीतर-भीतर जो बेलबूटे काढ़े गए थे, उनके सारे नक़्शे उन्होंने ही खींचे थे, और उनमें से एक-एक का काढ़ा जाना उनकी ही बारीक निगरानी में हुआ था।
मेरे मामाजी के बग़ीचे में शीशम, सखुए कटहल आदि इमारतों में काम आने वाले पेड़ों की भरमार थी। मस्जिद की सारी लकड़ी हमारे ही बग़ीचे से गई थी।
जिस दिन मस्जिद तैयार हुई थी, सुभान दादा ने जवार भर के प्रतिष्ठित लोगों को न्योता दिया था। जुमा का दिन था। जितने मुसलमान थे, सबने उसमें नमाज़ पढ़ी थी। जितने हिंदू आए थे, उनके सत्कार के लिए दादा ने हिंदू हलवाई रखकर तरह-तरह की मिठाइयाँ बनवाई थीं, पान-इलायची का प्रबंध किया था। अब तक भी लोग उस मस्जिद के उद्घाटन के दिन की दादा की मेहमानदारी भूले नहीं हैं।
ज़माना बदला। मैं अब शहरों में ही ज़ियादातर रहा और शहर आए दिन हिंदू-मुसलिम दंगों के अखाड़े बन जाते थे। हाँ, आए दिन देखिएगा, एक ही सड़क पर हिंदू-मुसलमान चल रहे हैं, एक ही दुकान पर सौदे ख़रीद रहे हैं, एक ही सवारियों पर ज़ानू-ब-ज़ानू आ-जा रहे हैं, एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं। एक ही दफ़्तर में काम कर रहे हैं कि अचानक सबके सिर पर शैतान सवार हो गया! हल्ला, भगदड़, मारपीट, ख़ूनख़राबा, आगज़नी, सारी ख़ुराफ़ातों की छूट! न घर महफ़ूज़, न शरीर, न इज़्ज़त! प्रेम भाईचारे और सहृदयता के स्थान पर घृणा, विरोध और नृशंस हत्या का उल्लंग नृत्य!
शहरों की यह बीमारी धीरे-धीरे देहात में घुसने लगी। गाय और बाजे के नाम पर तकरारें होने लगीं। जो ज़िंदगी भर क़साईख़ानों के लिए अपनी गायें बेचते रहे, वे ही एक दिन किसी एक गाय के कटने का नाम सुनकर ही कितने इंसानों के गले काटने को तैयार होने लगे। जिनके शादी-ब्याह, परब-त्यौहार बिना बाजे के नहीं होते, जो मुहर्रम की गर्मी के दिन भी बाजे-गाजों की धूम किए रहते, अब वे ही अपनी मस्जिद के सामने से गुज़रते हुए एक मिनट के बाजे पर ख़ून की नदियाँ बहाने को उतारू हो जाते!
कुछ पंडितों की बन आई, कुछ मुल्लाओं की चलती बनी। संगठन और तंज़ीम के नाम पर फूट और कलह के बीज बोए जाने लगे। लाठियाँ उछली, छुरे निकले। खोपड़ियाँ फूटीं, अंतड़ियाँ बाहर आईं। कितने नौजवान मरे, कितने घर फूँके! बाक़ी बच गए खेत-खलिहान, सो अँग्रेज़ी अदालत के ख़र्चे में पीछे कुर्क हुए।
ख़बर फैली, इस साल सुभान दादा के गाँव के मुसलमान भी क़ुर्बानी करेंगे। जवार में मुसलमान कम थे, लेकिन उनके जोश का क्या कहना? इधर हिंदुओं की जितनी गाय पर ममता न थी, उससे ज़ियादा अपनी तादाद पर घमंड था। तना-तनी का बाज़ार गर्म! ख़बर यह भी फैली कि सुभान ख़ाँ की मस्जिद में ही कुरबानी होगी।
एँ, सुभान ख़ाँ की मस्जिद में ही क़ुरबानी होगी! नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।”
“अगर हुई, तो क्या होगा? हमारी नाक कट जाएगी! लोग क्या कहेंगे, इतने हिंदू के रहते गो-माता के गले पर छुरी चली!'
छुरी से गो-माता को बचाना है तो गौरागौरी के क़साईख़ाने पर हम धावा करें? और, अगर सचमुच जोश है तो चलिए, मुज़फ़्फ़रपुर अँग्रेज़ी फ़ौज की छावनी पर ही धावा बोलें। क़साईख़ाने में तो बूढ़ी गायें कटती हैं, छावनी में तो मोटी-ताज़ी बछियाँ ही काटी जाती हैं।
लेकिन वे तो हमारी आँखों से दूर हैं देखते हुए मक्खी कैसे निगली जाएगी?
माफ कीजिए। दूर-नज़दीक की बात नहीं है। बात है हिम्मत की, ताक़त की। छावनी में आप नहीं जाते हैं, इसलिए कि वहाँ सीधे तोप के मुँह में पड़ना होगा यहाँ मुसलमान एक मुट्ठी हैं, इसलिए आप टूटने को उतावले हैं!”
“आप सुभान ख़ाँ का पक्ष ले रहे हैं, दोस्ती निभाते हैं! धर्म से बढ़कर दोस्ती नहीं।
कुछ नौजवानों को मेरे मामाजी की बातें ऐसी बुरी लगों कि सख़्त-सुस्त कहते वहाँ से उठकर चल दिए। लेकिन कितना भी ग़ुस्सा किया जाए, चीख़ा-चिल्लाया जाए, यह साफ़ बात है कि मामा की बिना रज़ामंदी के किसी बड़ी घटना के लिए किसी की पैर उठाने की हिम्मत नहीं हो सकती थी। उधर सुभान दादा के दरवाज़े पर भी मुसलमानों की भीड़ है न जाने दादा में कहाँ का जोश आ गया है। वह कड़कर कह रहे हैं—
गाय की क़ुरबानी नहीं होगी ये फ़ालतू बातें सुनने को मैं तैयार नहीं हूँ तुम लोग हमारी आँखों के सामने से हट जाओ।
क्यों नहीं होगी? क्या हम अपना मज़हब डर के मारे छोड़ देंगे?''
मैं कहता हूँ, यह मज़हब नहीं है। मैं हज से हो आया हूँ, क़ुरान मैंने पढ़ी है। गाय की क़ुरबानी लाज़िमी नहीं हैं। अरब में लोग दुंबे और ऊँट की क़ुरबानी उमूमन करते हैं।
लेकिन हम गाय की ही क़ुरबानी करें तो वे रोकनेवाले कौन होते हैं? हमारे मज़हब में वे दख़ल-अंदाज़ी क्यों करेंगे?
उनकी बात उनसे पूछो मैं मुसलमान हूँ, कभी अल्लाह को नहीं भूला हूँ। मैं मुसलमान की हैसियत से कहता हूँ, मैं गाय की क़ुरबानी न होने दूँगा, न होने दूँगा!
दादा की समूची दाढ़ी हिल रही थी, ग़ुस्से से चेहरा लाल था, होंठ फड़क रहे थे, शरीर तक हिल रहा था। उनकी यह हालत देख सभी चुप रहे। लेकिन एक नौजवान बोल उठा, आप बड़े हैं, आप अब अलग बैठिए। हम काफ़िरों से समझ लेंगे।
दादा चीख़ उठे, कल्लू के बेटे, ज़बान संभालकर बोल! तू किन्हें काफ़िर कह रहा है? और मेरे बुढ़ापे पर मत जा—मैं मस्जिद में चल रहा हूँ। पहले मेरी क़ुरबानी हो लेगी, तब गाय की कुरबानी हो सकेगी।
सुभान दादा वहाँ से उसी तनातनी की हालत में मस्जिद में आए। नमाज़ पढ़ी। फिर तसबीह लेकर मस्जिद के दरवाज़े की चौखट पर “मेरी लाश पर हो कर ही कोई भीतर घुस सकता है। कहकर बैठ गए। उनकी आँख मुँदी हैं, किंतु आँसुओं की झड़ी उनके गाल से होती, उनको दाढ़ी को भिगोती, अजस्त्र रूप में गिरती जा रही है। हाथ में तसबीह के दाने हिल रहे हैं और होंठों पर ज़रा ज़रा जुंबिश है। नहीं तो उनका समूचा शरीर संगमरमर की मूर्ति सा लग रहा है—निश्चल, निस्पंद धीरे-धीरे मस्जिद के नज़दीक लोग इकट्ठे होने लगे। पहले मुसलमान फिर हिंदू भी। अब गाय की क़ुरबानी का सवाल दादा की आँसुओं की धारा में बहकर न जाने कहाँ चला गया था! वह साक्षात् देवदूत से दीख पड़ते थे। देवदूत, जिसके रोम-रोम से प्रेम और भाईचारे का संदेश निकलकर वायुमंडल को व्याप्त कर रहा था।
अभी उस दिन मेरी रानी मेरे दो वर्ष जेल में जाने के बाद इतने लंबे अरसे तक राह देखती-देखती आख़िर मुझसे मिलने 'गया' सेंट्रल जेल में आई थी।
इतने दिनों की बिछुड़न के बाद मिलने पर जो सबसे पहली चीज़ उसने मेरे हाथों पर रखी ये थे रेशम और कुछ सूत के अजीब-ओ-ग़रीब ढंग से लिपटे लिपटाए डोरे, बुद्धियाँ, गंडे आदि। यह सूरत देवता के हैं, यह अनंत देवता के, यह ग्राम-देवता के यूँ ही गिनती गिनती, आख़िर में बोली, ये हुसैन साहब के गड़े हैं। आपको मेरी क़सम इन्हें ज़रूर ही पहन लीजिएगा।
ये सब मेरी माँ की मन्नतों के अवशेष चिह्न हैं। माँ चली गई। लेकिन तो भी ये मन्नतें अब भी निभाई जा रही हैं। रानी जानती हैं, मैं नास्तिक हूँ। इसलिए जब-जब इनके मौक़े आते हैं, ख़ुद इन्हें मेरे गले में डाल देती है। आज इस जेल में जेल कर्मचारियों और ख़ुफिया पुलिस के सामने उसने ऐसा नहीं किया, लेकिन क़सम देने से नहीं चूकी। मैंने भी हँसकर मानो उसकी दिलजमई कर दी।
रानी चली गई, लेकिन वे गंडे अब भी मेरे सूटकेस में संजोकर रखे हैं।
जब-जब सूटकेस खोलता हूँ और हुसैन साहब के उन गंडों पर नज़र पड़ती है, तब-तब दो अपूर्व तसवीर आँखों के सामने नाच जाती हैं—पहला कर्बला की; जिसमें एक और कुल मिलाकर सिर्फ़ बहत्तर आदमी हैं, जिनमें बच्चे और औरतें भी हैं। इस छोटी सी जमात के सरदार हैं हजरत हुसैन साहब! इन्हें बार-बार आग्रह करके बुलाया गया था—कूफ़ा की गद्दी पर बिठलाने के लिए। लेकिन गद्दी पर बिठाने के बदले आज उनके लिए एक चुल्लू पानी का मिलना भी मुहाल कर दिया गया है। सामने फ़रात नदी बह रही है, लेकिन उसके घाट-घाट पर पहरे हैं, उन्हें पानी लेने नहीं दिया जा रहा है। कहा जाता है—'दुराचारी, दुराग्रही यज़ीद की सत्ता क़बूल करो, नहीं तो प्यासे तड़पकर मरो' बच्चे प्यास के मारे बिलबिला रहे हैं; उनकी माँ और बहनें तड़प रही हैं। हाय रे, एक चुल्लू पानी मेरे लाल के कंठ सूखे जा रहे हैं, उसकी साँस रुकी है। पानी, एक चुल्लू पानी!
पानी की तो नदी बह रही है और तुम्हें इज़्ज़त और दौलत भी कम नहीं बख़्शी जाएगी, क्योंकि तुम ख़ुद रसूल जो हो। लेकिन, शर्त यह है कि यज़ीद के हाथ पर बैत करो।
यज़ीद के हाथ पर बेत? दुराचारी, दुराग्रही यज़ीद की सत्ता क़बूल करने और रसूल का नवासा? हो नहीं सकता हम एक चुल्लू पानी में डूब मरना पसंद करेंगे, लेकिन यह नीच काम रसूल के नाती से नहीं होगा।
लेकिन, बच्चों के लिए तो पानी लाना ही है। उन्हें यूँ जीते जी तड़पकर मरने नहीं दिया जा सकता!
एक और बहत्तर आदमी, जिसमें बच्चे और स्त्रियाँ भी, दूसरी ओर दुराचारी यज़ीद की अपार सजी-सजाई फ़ौज! लड़ाई होती है, हज़रत हुसैन और उनका पूरा क़ाफ़िला उस कर्बला के मैदान में शहादत पाता है। शहीदों के रक्त से उस सहरा के रजकण लाल हो उठते हैं, बच्चों की तड़प और अबलाओं की चीख़ से वातावरण थर्रा उठता है। इतनी बड़ी दर्दनाक घटना संसार के इतिहास में मिलना मुश्किल है। मुहर्रम उसी दिन का करुण स्मारक हैं। संसार के कोने-कोने में यह स्मारक हर मुसलमान मनाता है। भाईचारा बढ़ाने पर हिंदुओं ने भी इसे अपना त्योहार बना लिया था, जो सब तरह ही योग्य था।
और दूसरी तसवीर सुभान दादा की—
जिनके कंधे पर चढ़कर मैं मुहर्रम देखने जाया करता था। वह चौड़ी पेशानी, वह सफ़ेद दाढ़ी वै ममता भरी आँखें, वे शहद टपकाने वाले होंठ, उनका यह नूरानी चेहरा! जिनकी जवानी अल्लाह और काम के बीच बराबर हिस्से में बँटी थी! जिनके दिमाग़ में आला ख़याल थे और हृदय में प्रेम की धारा लहराती थी! वह प्रेम की धारा—जो अपने पराए सबको समान रूप से शीतल करती और सींचती है।
मेरा सिर सिज्दे में झुका है—कर्बला के शहीद के सामने! मैं सप्रेम नमस्कार करता हूँ—अपने प्यारे सुभान दादा को!
=======================
रज़िया / माटी की मूरतें /रामवृक्ष बेनीपुरी
रज़िया
पुस्तक : माटी की मूरतें
रचनाकार : रामवृक्ष बेनीपुरी
कानों में चाँदी की बालियाँ, गले में चाँदी का हैकल, हाथों में चाँदी के कंगन और पैरों में चाँदी की गोड़ाई—भरबाँह की बूटेदार क़मीज़ पहने, काली साड़ी के छोर को गले में लपेटे, गोरे चेहरे पर लटकते हुए कुछ बालों को सँभालने में परेशान वह छोटी सी लड़की जो उस दिन मेरे सामने आकर खड़ी हो गई थी—अपने बचपन की उस रज़िया की स्मृति ताज़ा हो उठी, जब मैं अभी उस दिन अचानक उसके गाँव में जा पहुँचा।
हाँ, यह मेरे बचपन की बात है। मैं क़साईख़ाने से रस्सी तुड़ाकर भागे हुए बछड़े की तरह उछलता हुआ अभी-अभी स्कूल से आया था और बरामदे की चौकी पर अपना बस्ता स्लेट पटककर मौसी से छठ में पके ठेकुए लेकर उसे कुतर-कुतर कर खाता हुआ ढेंकी पर झूला झूलने का मज़ा पूरा करना चाह रहा था कि उधर से आवाज़ आई—'देखना, बबुआ का खाना छू मत देना। और उसी आवाज़ के साथ मैंने देखा, यह अजीब रूप-रंग की लड़की मुझसे दो-तीन गज़ आगे खड़ी हो गई।
मेरे लिए यह रूप-रंग सचमुच अजीब था। ठेठ हिंदुओं की बस्ती है मेरी और मुझे मैले पेटिए में भी अधिक नहीं जाने दिया जाता। क्योंकि सुना है, बचपन में मैं एक मेले में खो गया था। मुझे कोई औघड़ लिए जा रहा था कि गाँव की एक लड़की की नज़र पड़ी और मेरा उद्धार हुआ। मैं माँ-बाप का इकलौता—माँ चल बसी थीं। इसलिए उनकी इस एकमात्र धरोहर को मौसी आँखों में जुगोकर रखती। मेरे गाँव में भी लड़कियों की कमी नहीं; किंतु न उनकी यह वेश-भूषा, न यह रूप-रंग मेरे गाँव की लड़कियाँ कानों में बालियाँ कहाँ डालती और भरबाँह की क़मीज़ पहने भी उन्हें कभी नहीं देखा और गोरे चेहरे तो मिले हैं, किंतु इसकी आँखों में जो एक अजीब क़िस्म का नीलापन दीखता, वह कहाँ? और, समुचे चेहरे की काट भी कुछ निराली ज़रूर तभी तो मैं उसे एकटक घूरने लगा।
यह बोली थी रज़िया की माँ, जिसे प्रायः ही अपने गाँव में चूड़ियों की खँचिया लेकर आते देखता आया था। वह मेरे आँगन में चूड़ियों का बाज़ार पसारकर बैठी थीं और कितनी बहू-बेटियाँ उसे घेरे हुई थीं। मुँह से भाव-साव करती और हाथ से ख़रीदारों के हाथ में चूड़ियाँ चढ़ाती वह सौदे पटाए जा रही थी। अब तक उसे अकेले ही आते-जाते देखा था; हाँ, कभी-कभी उसके पीछे कोई मर्द होता जो चूड़ियों की खाँची ढोता। यह बच्ची आज पहली बार आई थी और न जाने किस बाल-सुलभ उत्सुकता ने उसे मेरी ओर खींच लिया था। शायद वह यह भी नहीं जानती थी कि किसी के हाथ का खाना किसी के निकट पहुँचने से ही छू जाता है। माँ जब अचानक चीख़ उठी, वह ठिठकी सहमी—उसके पैर तो वहीं बँध गए। किंतु इस ठिठक ने उसे मेरे बहुत निकट ला दिया, इसमें संदेह नहीं।
मेरी मौसी झट उठी, घर में गई और दो ठेकुए और एक कसार लेकर उसके हाथों में रख दिए। वह लेती नहीं थी, किंतु अपनी माँ के आग्रह पर हाथ में रख तो लिया, किंतु मुँह से नहीं लगाया! मैंने कहा—खाओ! क्या तुम्हारे घरों में से सब नहीं बनते? छठ का व्रत नहीं होता? कितने प्रश्न—किंतु सबका जवाब 'न' में ही और वह भी मुँह से नहीं, ज़रा सा गरदन हिलाकर और गरदन हिलाते ही चेहरे पर गिरे बाल की जो लटें हिल-हिल उठती, वह उन्हें परेशानी से संभालने लगती।
जब उसकी माँ नई ख़रीदारिनों की तलाश में मेरे आँगन से चली, रज़िया भी उसके पीछे हो लो। में खाकर, मुँह धोकर अब उसके निकट था और जब वह चली, जैसे उसकी डोर में बँधा थोड़ी दूर तक घिसटता गया। शायद मेरी भावुकता देखकर ही चूड़ीहारिनों के मुँह पर खेलने वाली अजस्त्र हँसी और चुहल में ही उसकी माँ बोली—बबुआजी, रज़िया से ब्याह कीजिएगा? फिर बेटी की और मुख़ातिब होती मुस्कुराहट में कहा—क्यों रे रज़िया, यह दुलहा तुम्हें पसंद है? उसका यह कहना कि मैं मुड़कर भागा ब्याह? एक मुसलमानिन से? अब रज़िया की माँ ठठा रही थी और रज़िया सिमटकर उसके पैरों में लिपटी थी, कुछ दूर निकल जाने पर मैंने मुड़कर देखा।
रज़िया, चूड़ीहारिन! वह इसी गाँव की रहनेवाली थी। बचपन में इसी गाँव में रही और जवानी में भी। क्योंकि मुसलमानों की गाँव में भी शादी हो जाती है न! और यह अच्छा हुआ—क्योंकि बहुत दिनों तक प्राय: उससे अपने गाँव में ही भेंट हो जाया करती थी।
मैं पढ़ते-पढ़ते बढ़ता गया। पढ़ने के लिए शहरों में जाना पड़ा। छुट्टियों में जब-तब आता इधर रज़िया पढ़ तो नहीं सकी, हाँ, बढ़ने में मुझसे पीछे नहीं रही। कुछ दिनों तक अपनी माँ के पीछे-पीछे घूमती फिरी। अभी उसके सिर पर चूड़ियों की खँचिया तो नहीं पड़ी, किंतु ख़रीदारिनों के हाथों में चूड़ियाँ पहनाने की कला वह जान गई थी। उसके हाथ मुलायम हैं, बहुत मुलायम नई बहुओं की यही राय थी। वे उसी के हाथ से चूड़ियाँ पहनना पसंद करतीं। उसकी माँ इससे प्रसन्न ही हुई—जब तक रज़िया चूड़ियाँ पहनाती, वह नई-नई ख़रीदारिनें फँसाती।
रज़िया बढ़ती गई। जब-जब भेंट होती, मैं पाता, उसके शरीर में नए-नए विकास हो रहे हैं; शरीर में और स्वभाव में भी। पहली भेंट के बाद पाया था, वह कुछ प्रगल्भ हो गई है। मुझे देखते ही दौड़कर निकट आ जाती, प्रश्न पर प्रश्न पूछती। अजीब अटपटे प्रश्न! देखिए तो ये नई बालियाँ आपको पसंद हैं? क्या शहरों में ऐसी ही बालियाँ पहनी जाती हैं? मेरी माँ शहर से चुड़ियाँ लाती है, मैंने कहा है, वह इस बार मुझे भी ले चलें। आप किस तरफ़ रहते हैं वहाँ? क्या भेंट हो सकेगी? वह बके जाती, मैं सुनता जाता! शायद जवाब की ज़रूरत यह भी नहीं महसूस करती।
फिर कुछ दिनों के बाद पाया, वह अब कुछ सकुचा रही है। मेरे निकट आने के पहले वह इधर-उधर देखती और जब कुछ बातें करती तो ऐसी चौकन्नी-सी कि कोई देख न ले, सुन न ले। एक दिन जब वह इसी तरह बातें कर रही थी कि मेरी भौजी ने कहा—देखियो री रज़िया बबुआजी को फुसला नहीं लीजियो। वह उनकी और देखकर हँस तो पड़ी, किंतु मैंने पाया, उसके दोनों गाल लाल हो गए हैं और उन नीली आँखों के कोने मुझे सजल-से लगे। मैंने तब से ध्यान दिया, जब हम लोग कहीं मिलते हैं, बहुत सी आँखें हम पर भालों की नौक ताने रहती हैं।
रज़िया बढ़ती गई, बच्चों से किशोरी हुई और अब जवानी के फूल उसके शरीर पर खिलने लगे हैं। अब भी वह माँ के साथ ही आती है; किंतु पहले वह माँ की एक छाया मात्र लगती थी, अब उसका स्वतंत्र अस्तित्व है। और उसकी छाया बनने के लिए कितनों के दिलों में कसमसाहट है जब वह बहनों को चूड़ियाँ पहनाती होती है, कितने भाई तमाशा देखने को वहाँ एकत्र हो जाते हैं। क्या? बहनों के प्रति अतृभाव या रज़िया के प्रति अज्ञात आकर्षण उन्हें खींच लाता है? जब वह बहुओं के हाथों में चूड़ियाँ ठेलती होती है, पतिदेव दूर खड़े कनखियों से देखते रहते हैं। क्या? अपनी नवोढ़ा की कोमल कलाइयों पर कोड़ा करती हुई रज़िया की पतली उँगलियों को! और, रज़िया को इसमें रस मिलता है। पतियों से चुहले करने से भी वह बाज़ नहीं आती—बाबू बड़ी महीन चूडियाँ हैं! ज़रा देखिएगा, कहीं चटक न जाएँ! पतिदेव भागते हैं, बहुएँ खिलखिलाती हैं। रज़िया ठट्ठा लगाती है। अब वह अपने पेशे में निपुण होती जाती है।
हाँ, रज़िया अपने पेशे में भी निपुण होती जाती थी। चूड़ीहारिन के पेशे के लिए सिर्फ़ यही नहीं चाहिए कि उसके पास रंग-बिरंगी चूड़ियाँ हों—सस्ती, टिकाऊ, टटके-से-टटके फैशन की। बल्कि यह पेशा चूड़ियों के साथ चूड़ीहारिनों में बनाव-शृंगार रूप-रंग, नाज़-ओ-अदा भी खोजता है, जो चूड़ी पहननेवालियों को ही नहीं, उनको भी मोह सके, जिनकी जेब से चूड़ियों के लिए पैसे निकलते हैं। सफल चूड़ीहारिन यह रज़िया की माँ भी किसी ज़माने में क्या कुछ कम रही होगी! खंडहर कहता है, इमारत शानदार थी!
ज्यों-ज्यों शहर में रहना बढ़ता गया, रज़िया से भेंट भी दुर्लभ होती गई और एक दिन वह भी आया, जब बहुत दिनों पर उसे अपने गाँव में देखा। पाया, उसके पीछे एक नौजवान चूड़ियों की खाँची सिर पर लिए है। मुझे देखते ही वह सहमी, सिकुड़ी और मैंने मान लिया, यह उसका पाति है। किंतु तो भी अनजान-सा पूछ ही लिया—इस जमूरे को कहाँ से उठा लाई है रे? इसी से पूछिए, साथ लग गया तो क्या करूँ? नौजवान मुस्कुराया, रज़िया भी हँसी, बोली यह मेरा ख़ाविंद है, मालिक!
ख़ाविंद! बचपन की उस पहली मुलाक़ात में उसकी माँ ने दिल्लगी-दिल्लगी में जो कह दिया था, न जाने, वह बात कहाँ सोई पड़ी थी! अचानक वह जगी और मेरी पेशानी पर उस दिन शिकन ज़रूर उठ आए होंगे, मेरा विश्वास है और एक दिन वह भी आया कि मैं भी ख़ाविंद बना! मेरी रानी को सुहाग की चूड़ियाँ पहनाने उस दिन यही रज़िया आई, और उस दिन मेरे आँगन में कितनी धूम मचाई इस नटखट ने यह लूँगी वह लूँगी और ये मुँहमाँगी चीज़ें नहीं मिलीं तो वह लूँगी कि दुलहन टापती रह जाएँगी! हट हट, तू बबुआजी को ले जाएगी तो फिर तुम्हारा यह हसन क्या करेगा? भौजी ने कहा। यह भी टापता रहेगा बहुरिया, कहकर रज़िया ठट्ठा मारकर हँसी और दौड़कर हसन से लिपट गई। ओहो, मेरे राजा, कुछ दूसरा न समझना हसन भी हँस पड़ा। रज़िया अपनी प्रेमकथा सुनाने लगी किस तरह यह हसन उसके पीछे पड़ा, किस तरह झंझटें आईं, फिर किस तरह शादी हुई और वह आज भी किस तरह छाया-सा उसके पीछे घूमता है। न जाने कौन सा डर लगा रहता है इसे? और फिर, मेरी रानी की कलाई पकड़कर बोली—मालिक भी तुम्हारे पीछे इसी तरह छाया की तरह डोलते रहें, दुलहन! सारा आँगन हँसी से भर गया था और उस हँसी में रज़िया के कानों की बालियों ने अजीब चमक भर दी थी, मुझे ऐसा ही लगा था।
जीवन का रथ खुरदरे पथ पर बढ़ता गया। मेरा भी रज़िया का भी। इसका पता उस दिन चला, जब बहुत दिनों पर उससे अचानक पटना में भेंट हो गई। यह अचानक भेंट तो थी; किंतु क्या इसे भेंट कहा जाए?
मैं अब ज़ियादातर घर से दूर-दूर ही रहता। कभी एकाध दिन के लिए घर गया तो शाम को गया, सुबह भागा। तरह-तरह की ज़िम्मेदारियाँ तरह-तरह के जंजाल! इन दिनों पटना में था, यूँ कहिए, पटना सिटी में एक छोटे से अख़बार में था—पीर-बावर्ची-भिश्ती की तरह! यो जो लोग समझते कि मैं संपादक ही हूँ। उन दिनों न इतने अख़बार थे, न इतने संपादक। इसलिए मेरी बड़ी क़दर है, यह मैं तब जानता जब कभी दफ़्तर से निकलता। देखता, लोग मेरी ओर उँगली उठाकर फुसफुसा रहे हैं। लोगों का मुझ पर यह ध्यान—मुझे हमेशा अपनी पद-प्रतिष्ठा का ख़याल रखना पड़ता।
एक दिन मैं चौक के एक प्रसिद्ध पानवाले की दुकान पर पान खा रहा था। मेरे साथ मेरे कुछ प्रशंसक युवक थे। एक-दो बुज़ुर्ग भी आकर खड़े हो गए। हम पान खा रहे थे और कुछ चुहलें चल रही थीं कि एक बच्चा आया और बोला, 'बाबू, वह औरत आपको बुला रही है।'
औरत! बुला रही है? चौक पर! मैं चौंक पड़ा। युवकों में थोड़ी हलचल, बुज़ुगों के चेहरों पर की रहस्यमयी मुस्कान भी मुझसे छिपी नहीं रही। औरत! कौन? मेरे चेहरे पर ग़ुस्सा था, वह लड़का सिटपिटाकर भाग गया।
पान खाकर जब लोग इधर-उधर चले गए, अचानक पाता हूँ, मेरे पैर उसी और उठ रहे हैं, जिस और उस बच्चे ने उँगली से इशारा किया था। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर पीछे देखा, परिचितों में से कोई देख तो नहीं रहा है। किंतु इस चौक की शाम की रूमानी फ़िज़ा में किसी को किसी की ओर देखने की कहाँ फ़ुरसत! मैं आगे बढ़ता गया और वहाँ पहुँचा, जहाँ उससे पूरब वह पीपल का पेड़ है। वहाँ पहुँच ही रहा था कि देखा, पेड़ के नीचे चबूतरे की तरफ़ से एक स्त्री बढ़ी आ रही है और निकट पहुँचकर यह कह उठी 'सलाम मालिक!'
धक्का-सा लगा, किंतु पहचानते देर नहीं लगी—उसने ज्यों ही सिर उठाया, चाँदी की बालियाँ जो चमक उठीं!
'रज़िया! यहाँ कैसे?' मेरे मुँह से निकल पड़ा।
'सौदा-सुलफ करने आई हूँ, मालिक! अब तो नए क़िस्म के लोग हो गए न? अब लाख की चूडियाँ कहाँ किसी को भाती हैं। नए लोग, नई चूड़ियाँ! साज-सिंगार की कुछ और चीज़ें भी ले जाती हूँ—पॉडर, किलप, क्या क्या चीज़ें हैं न। नया ज़माना, दुलहनों के नए-नए मिजाज!’
फिर ज़रा सा रुककर बोली, 'सुना था, आप यहाँ रहते हैं, मालिका में तो अकसर आया करती हूँ।’
और यह जब तक पूछें कि अकेली हो या कि एक अधवयस्क आदमी ने आकर सलाम किया। यह हसन था। लंबी-लंबी दाढ़ियाँ, पाँच हाथ का लंबा आदमी, लंबा और मुस्टंडा भी। 'देखिए मालिक, यह आज भी मेरा पीछा नहीं छोड़ता!' यह कहकर रज़िया हँस पड़ी। अब रज़िया वह नहीं थी, किंतु उसकी हँसी नहीं थी। वही हँसी, वही चुहल! इधर-उधर की बहुत सी बातें करती रही और न जाने कब तक जारी रखती कि मुझे याद आया, मैं कहाँ खड़ा हूँ और अब मैं कौन हूँ कोई देख ले तो?
किंतु वह फ़ुरसत दे तब न! जब मैंने जाने की बात की, हसन की ओर देखकर बोली, 'क्या देखते हो, ज़रा पान भी तो मालिक को खिलाओ। कितनी बार हुमच-हुमचकर भरपेट ठूँस चुके हो बाबू के घर।'
जब हसन पान लाने चला गया, रज़िया ने बताया कि किस तरह दुनिया बदल गई है। अब तो ऐसे भी गाँव हैं, जहाँ के हिंदू मुसलमानों के हाथ से सौदे भी नहीं ख़रीदते। अब हिंदू चूड़ीहारिने हैं, हिंदू दर्ज़ी हैं। इसलिए रज़िया जैसे ख़ानदानी पेशेवालों को बड़ी दिक़्क़त हो गई है। किंतु, रज़िया ने यह ख़ुशख़बरी सुनाई—मेरे गाँव में यह पागलपन नहीं, और मेरी रानी तो सिवा रज़िया के किसी दूसरे के हाथ से चूड़ियाँ लेती ही नहीं।
हसन का लाया पान खाकर जब मैं चलने को तैयार हुआ, वह पूछने लगी, 'तुम्हारा डेरा कहाँ है?' मैं बड़े पशोपेश में पड़ा। 'डरिए मत मालिक, अकेले नहीं आऊँगी, यह भी रहेगा। क्यों मेरे राजा?' यह कहकर वह हसन से लिपट पड़ी 'पगली, पगली, यह शहर है, शहर!' यूँ हसन ने हँसते हुए बाह छुड़ाई और बोला, 'बाबू, बाल बच्चोंवाली हो गई, किंतु इसका बचपना नहीं गया।'
और दूसरे दिन पाता हूँ, रज़िया मेरे डेरे पर हाज़िर है! 'मालिक, ये चूड़ियाँ रानी के लिए।' कहकर मेरे हाथों में चूड़ियाँ रख दी।
मैंने कहा, 'तुम तो घर पर जाती ही हो, लेतो जाओ, वहीं दे देना।'
नहीं मालिक, एक बार अपने हाथ से भी पिनहाकर देखिए!' कह खिलखिला पड़ी। और जब मैंने कहा, 'अब इस उम्र में?' तो वह हसन की ओर देखकर बोली, पूछिए इससे आज तक मुझे यही चूड़ियाँ पिनहाता है या नहीं?' और, जब हसन कुछ शरमाया, वह बोली, 'घाघ है मालिक, घाघ! कैसा मुँह बना रहा है इस समय! लेकिन जब हाथ-में-हाथ लेता है,' ठठाकर हँस पड़ी, इतने ज़ोर से कि मैं चौंककर चारों तरफ़ देखने लगा।
हाँ, तो अचानक उस दिन उसके गाँव में पहुँच गया। चुनाव का चक्कर—जहाँ न ले जाए, जिस औघट-घाट पर न खड़ा कर दें! नाक में पेट्रोल के धुएँ की गंध, कान में साँय-साँय की आवाज़, चेहरे पर गरद-ग़ुबार का अंबार परेशान, बदहवास; किंतु उस गाँव में ज्यों ही मेरी जीप घुसी, मैं एक ख़ास क़िस्म की भावना से अभिभूत हो गया।
यह रज़िया का गाँव है। यहाँ रज़िया रहती थी। किंतु क्या आज मैं यहाँ यह भी पूछ सकता हूँ कि यहाँ कोई रज़िया नाम की चूड़ीहारिन रहती थी, या है? हसन का नाम लेने में भी शर्म लगती थी। मैं वहाँ नेता बनकर गया था, मेरी जय-जयकार हो रही थी। कुछ लोग मुझे घेरे खड़े थे। जिसके दरवाज़े पर जाकर पान खाऊँगा, वह अपने को बड़भागी समझेगा जिससे दो बातें कर लूँगा, वह स्वयं चर्चा का एक विषय बन जाएगा। इस समय मुझे कुछ ऊँचाई पर ही रहना चाहिए।
जीप से उतरकर लोगों से बातें कर रहा था, या यूँ कहिए कि कल्पना के पहाड़ पर खड़े होकर एक आने वाले स्वर्ण युग का संदेश लोगों को सुना रहा था, किंतु दिमाग़ में कुछ गुत्थियाँ उलझी थीं। जीभ अभ्यासवश एक काम किए जा रही थी, अंतर्मन कुछ दूसरा ही ताना-बाना बुन रहा था। दोनों में कोई तारतम्य न था; किंतु इसमें से किसी एक की गति में भी क्या बाधा डाली जा सकती थी?
कि अचानक लो, यह क्या? वह रज़िया चली आ रही है! रज़िया! वह बच्ची, अरे, रज़िया फिर बच्ची हो गई? कानों में वे ही बालियाँ, गोरे चेहरे पर वे ही नीली आँखें, वही भरबाँह की क़मीज़, वे ही कुछ लटें, जिन्हें सँभालती बढ़ी आ रही है। बीच में चालीस पैंतालीस साल का व्यवधान! अरे, मैं सपना तो नहीं देख रहा? दिन में सपना! वह आती है, जबरन ऐसी भीड़ में घुसकर मेरे निकट पहुँचती हैं, सलाम करती हैं और मेरा हाथ पकड़कर कहती है, 'चलिए मालिक, मेरे घर।'
मैं भौचक्का, कुछ सूझ नहीं रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा! लोग मुस्कुरा रहे हैं नेताजी, आज आपकी कलई खुलकर रही! नहीं, यह सपना है! कि कानों में सुनाई पड़ा, कोई कह रहा है—कैसी शोख़ लड़की! और दूसरा बोला—ठीक अपनी दादी जैसी! और तीसरे ने मेरे होश की दवा दी—यह रज़िया की पोती है, बाबू! बेचारी बीमार पड़ी है। आपकी चर्चा अकसर किया करती है। बड़ी तारीफ` करती है। बाबू, फुरसत हो तो ज़रा देख लीजिए, न जाने बेचारी जीती है या...
मैं रज़िया के आँगन में खड़ा हूँ। ये छोटे-छोटे साफ़-सुथरे घर, यह लिपा पुता चिक्कन ढुर-ढुर आँगन! भरी-पूरी गृहस्थी—मेहनत और दयानत की देन। हसन चल बसा है, किंतु अपने पीछे तीन हसन छोड़ गया है। बड़ा बेटा कलकत्ता कमाता है, मँझला पुश्तैनी पेशे में लगा है, छोटा शहर में पढ़ रहा है। यह बच्ची बड़े बेटे की बेटी। दादा का सिर पोते में, दादी का चेहरा पोती में। बहू रज़िया! यह दूसरी रज़िया मेरी उँगली पकड़े पुकार रही है—दादी, ओ दादी! घर से निकल मालिक दादा आ गए! किंतु पहली 'वह' रज़िया निकल नहीं रहीं। कैसे निकले? बीमारी के मैले कुचैले कपड़े में मेरे सामने कैसे आवे?
रज़िया ने अपनी पोती को भेज दिया, किंतु उसे विश्वास न हुआ कि हवागाड़ी पर आनेवाले नेता अब उसके घर तक आने की तकलीफ़ कर सकेंगे? और, जब सुना, मैं आ रहा हूँ तो बहुओं से कहा—ज़रा मेरे कपड़े तो बदलवा दो—मालिक से कितने दिनों पर भेंट हो रही है न!
उसकी दोनों पतोहुएँ उसे सहारा देकर आँगन में ले आई रज़िया—हाँ, मेरे सामने रज़िया खड़ी थी दुबली-पतली, रूखी-सूखी। किंतु जब नज़दीक आकर उसने 'मालिक, सलाम' कहा, उसके चेहरे से एक क्षण के लिए झुर्रियाँ कहाँ चली गई, जिन्होंने उसके चेहरे को मकड़जाला बना रखा था। मैंने देखा, उसका चेहरा अचानक बिजली के बल्ब की तरह चमक उठा और चमक उठीं वे नीली आँखें, जो कोटरों में धँस गई थीं! और, अरे चमक उठी हैं आज फिर वे चाँदी की बालियाँ और देखो, अपने को पवित्र कर लो! उसके चेहरे पर फिर अचानक लटककर चमक रही हैं वे लटें, जिन्हें समय ने धो-पोंछकर शुभ-श्वेत बना दिया है।
==========================