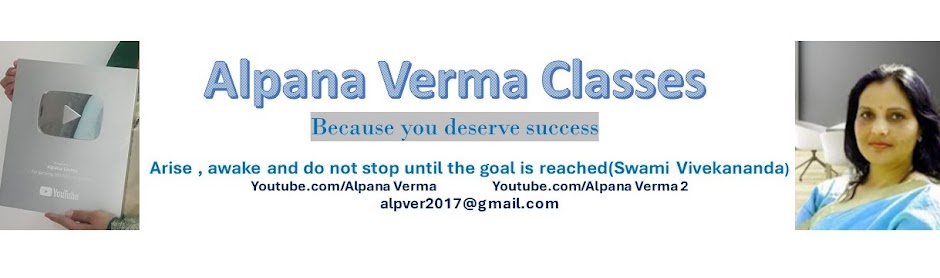======================
बादलों के घेरे
लेखिका :कृष्णा सोबती
भुवाली की इस छोटी-सी कॉटेज में लेटा-लेटा मैं सामने के पहाड़ देखता हूँ। पानी-भरे, सूखे-सूखे बादलों के घेरे देखता हूँ। बिना आँखों के झटक-झटक जाती धुंध के निष्फल प्रयास देखता हूँ और फिर लेटे-लेटे अपने तन का पतझार देखता हूँ। सामने पहाड़ के रूखे हरियाले में रामगढ़ जाती हुई पगडंडी मेरी बाँह पर उभरी लंबी नस की तरह चमकती है। पहाड़ी हवाएँ मेरी उखड़ी-उखड़ी साँस की तरह कभी तेज़, कभी हौले, इस खिड़की से टकराती हैं; पलंग पर बिछी चद्दर और ऊपर पड़े कंबल से लिपटी मेरी देह चूने की-सी कच्ची तह की तरह घुल-घुल जाती है। और बरसों के ताने-बाने से बुनी मेरे प्राणों की धड़कनें हर क्षण बंद हो जाने के डर में चूक जाती हैं।
मैं लेटा रहता हूँ और सुबह हो जाती है। मैं लेटा रहता हूँ शाम हो जाती है। मैं लेटा रहता हूँ रात झुक जाती है। दरवाज़े और खिड़कियों पर पड़े परदे मेरी ही तरह दिन-रात, सुबह-शाम, अकेले मौन-भाव से लटकते रहते हैं। कोई इन्हें भरे-भरे हाथों से उठाकर कमरे की ओर बढ़ा नहीं आता। कोई इस देहरी पर अनायास मुसकराकर खड़ा नहीं हो जाता। रात, सुबह, शाम बारी-बारी से मेरी शय्या के पास घिर-घिर आते हैं और मैं अपनी इन फीकी आँखों से अँधेरे और उजाले को नहीं, लोहे के पलंग पर पड़े अपने-आपको देखता हूँ, अपने इस छूटते-छूटते तन को देखता हूँ। और देखकर रह जाता हूँ। आज इस तरह जाने के सिवाय कुछ भी मेरे वश में नहीं रह गया। सब अलग जा पड़ा है। अपने कंधों से जुड़ी अपनी बाँहों को देखता हूँ, मेरी बाँहों में लगी वे भरी-भरी बाँहें कहाँ हैं...कहाँ हैं वे सुगंध-भरे केश, जो मेरे वक्ष पर बिछ-बिछ जाते थे? कहाँ हैं वे रस-भरे अधर जो मेरे रस में भीग-भीग जाते थे? सब था, मेरे पास सब था। बस, मैं आज-सा नहीं था। जीने का संग था, सोने का संग था और उठने का संग था। मैं धुले-धुले सिरहाने पर सिर डालकर सोता रहता और कोई हौले से चमककर कहता—उठोगे नहीं...भोर हो गई।